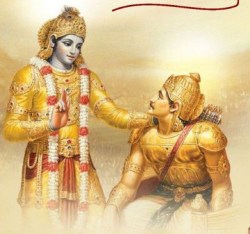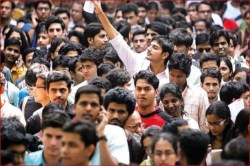Saturday, April 19, 2025
किशोरों का मन समझें, उन्हें नियंत्रक नहीं बल्कि दोस्त चाहिए
— अपर्णा पिरामल राजे
(‘केमिकल खिचड़ी : हाऊ आइ हैक्ड माइ मेंटल हेल्थ’ पुस्तक की लेखिका)
जयपुर•Apr 16, 2025 / 12:47 pm•
विकास माथुर
नेटफ्लिक्स की चर्चित सीरीज ‘एडोलसेंस’ ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इसकी कहानी में एक 13 साल के लड़के जैमी मिलर पर अपने ही सहपाठी की हत्या का आरोप है। यह कहानी जितनी चौंकाने वाली है, उतनी ही सच्चाई के करीब भी है। ब्रिटेन में बच्चों और किशोरों की मनोचिकित्सक रह चुकीं हीथर स्टुअर्ट की नजर में यह कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि आज के किशोरों की जटिल दुनिया को समझने का एक जरिया है। हीथर बताती हैं कि हम अक्सर कई किशोर लड़कों में हिंसा की झलक देखते हैं। एक बार मैंने एक लड़के को खतरनाक बताया था, लेकिन वह सिस्टम की निगरानी से बाहर चला गया और बाद में उसने दो लोगों की हत्या कर दी। वह मानती हैं कि सोशल मीडिया ने हालात को और मुश्किल कर दिया है।
संबंधित खबरें
आज बच्चे अपनी गुस्सैल भावनाओं को आसानी से जाहिर कर देते हैं, खासकर जब उन्हें एंड्रयू टेट जैसे लोग प्रभावित करते हैं। भारत में रहते हुए शायद हम सोचें कि ये हमारे समाज की नहीं, सिर्फ इंग्लैंड की सड़कों की कहानी है। लेकिन मुंबई की पारिवारिक थैरेपिस्ट मेघा सेखसरिया-मवांडिया इससे सहमत नहीं हैं। वह कहती हैं कि ये सीरीज आज के किशोरों की उस अदृश्य दुनिया को उजागर करती है, जो माता-पिता से छिपी रहती है। किशोरों की कोड भाषा, बदलती पहचान और वो दबाव, जिन्हें समझना माता-पिता के लिए आसान नहीं होता।
सीरीज के आखिरी एपिसोड में दिखाया गया है कि जैमी का अपराध उसके परिवार को कैसे तोड़ देता है। बतौर दो किशोरों की मां, लेखिका मानती हैं कि यह समय बच्चों से दूरी बनाने का नहीं, बल्कि उनके और करीब आने का है। छोटे बच्चों की देखभाल थकान भरी होती है, लेकिन जैसे-जैसे वे किशोरावस्था में कदम रखते हैं तो माता-पिता धीरे-धीरे उनका साथ कम करने लगते हैं। बच्चे या तो पढ़ाई और गतिविधियों में उलझ जाते हैं या अपनी डिजिटल दुनिया में खो जाते हैं। उदाहरण के लिए, मवांडिया का एक चौदह साल का क्लाइंट है,जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर (एडीएचडी) से पीडि़त है। हर बार स्कूल शिकायत करता है तो उसकी दवा की मात्रा बढ़ा दी जाती है।
पिता अपने काम और गोल्फ में व्यस्त हैं और मां को बच्चे की समस्याओं को सुलझाने का तरीका नहीं आता। नतीजन, वह अपने हमउम्र दोस्तों पर निर्भर हो जाता है, जो उसे गलत रास्तों पर ले जाते हैं। इसी तरह उनके पास लाया गया एक सोलह साल का लड़का अश्लील फिल्मों की लत से जूझ रहा था। उसकी मां को तब पता चला जब वह बात-बात पर गुस्से में बोलने लगा और पढ़ाई की बातें उनसे छिपाने लगा। मवांडिया कहती हैं कि बदलाव इतने छोटे होते हैं कि अगर हम सतर्क न रहें, तो वे नजर ही नहीं आते। हीथर स्टुअर्ट भी यही मानती हैं कि किशोरावस्था बचपन से जवानी की ओर बढऩे का संक्रमण काल है। इस समय में बच्चा अपने माता-पिता से अलग भी होता है, लेकिन जरूरत पडऩे पर उनके पास लौटना भी चाहता है।
माता-पिता को इन दोनों स्थितियों में संतुलन बनाना होता है। तो इन जटिल परिस्थितियों में किशोरों का साथ कैसे निभाया जाए? इसका एक ही उत्तर है कि अपने पालन-पोषण के तरीकों को बदलना। छोटे बच्चों को माता-पिता सही-गलत सिखाते हैं, नियम बनाते हैं और उनकी सुरक्षा करते हैं। लेकिन किशोरों को आजादी की ओर बढऩे देना होता है। वे अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, अपने फैसले खुद लेना चाहते हैं। ऐसे में माता-पिता को एक मार्गदर्शक और दोस्त की भूमिका निभानी होगी-एक कोच की तरह। जैसे एक कोच खिलाड़ी की जगह खेलता नहीं, लेकिन उसे खेलना सिखाता है, उसका मनोबल बढ़ाता है, गलतियों से सीखने में मदद करता है वैसे ही माता-पिता को किशोरों को जीवन जीने की कला सिखानी चाहिए।
मान लीजिए, अगर कोई किशोर खाना बनाने, एस्ट्रोफिजिक्स, डिजाइन या शेयर बाजार जैसी अलग-अलग चीजों में रुचि लेता है, तो माता-पिता को चाहिए कि उसकी हौसलाअफजाई करें, उसे सही लोगों से जोड़ें और उसकी जिज्ञासा को ‘बेमतलब’ कहकर खारिज न करें। जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उसी तरह माता-पिता को भी बदलना पड़ता है। उन्हें खुद को ‘आदेश देने वाले’ से ‘साथ चलने वाले’ में बदलना पड़ता है। यह बदलाव कुछ इस तरह होता है-नेता से श्रोता बनना, नियंत्रण से संवाद की ओर बढऩा, सुरक्षा देने से उन्हें तैयार करने तक जाना। यह कठिन लग सकता है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि दुनिया में जैमी मिलर जैसे और बच्चे न बनें, तो यह बदलाव बेहद जरूरी है और संभव भी है।
Hindi News / Opinion / किशोरों का मन समझें, उन्हें नियंत्रक नहीं बल्कि दोस्त चाहिए
यह खबरें भी पढ़ें
लेटेस्ट ओपिनियन न्यूज़
Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.