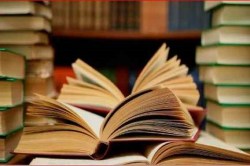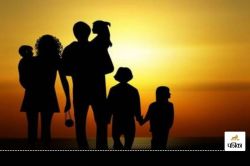Sunday, July 20, 2025
जलभराव के दौरान सतर्कता ही सबसे बड़ी सुरक्षा
रिपुन्जय सिंह
जयपुर•Jul 19, 2025 / 07:26 pm•
Neeru Yadav
शहरीकरण की तेज गति और जलवायु परिवर्तन के युग में शहरी बाढ़ एक सामान्य आपदा बनती जा रही है। यह न केवल भौतिक ढांचे को प्रभावित करती है, बल्कि शहर में रहने वाले लाखों लोगों के जीवन को भी अस्त-व्यस्त कर देती है। शहरी बाढ़ का प्रभाव सीधा नागरिकों की आजीविका, स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति, आवागमन, सुरक्षा तथा सामाजिक ताने-बाने पर पड़ता है। सडक़ों पर जलभराव से दैनिक जीवन शैली प्रभावित होती है। नागरिकों को घर से बाहर निकलने में कठिनाई, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस जाने वालों को बाधा उत्पन्न होती है। परिवहन व्यवस्था ठप होने से बसें, मेट्रो, टैक्सी सेवाएं बंद हो जाती हैं। घंटों लंबा ट्रैफिक जाम लग जाता है। बिजली और इंटरनेट बाधित होते हैं, घरों और दफ्तरों में कामकाज रुक जाता है। खरीदारी और घरेलू गतिविधियां रुक जाती हैं, बाजार बंद, रसोई गैस, सब्जियां, दूध और अन्य जरूरी चीजें उपलब्ध नहीं होतीं।
शहरी बाढ़ आधुनिक शहरों की एक गंभीर समस्या बन चुकी है। तेजी से होते शहरीकरण, असंतुलित विकास और जलवायु परिवर्तन के चलते बाढ़ की घटनाएं न केवल आम होती जा रही हैं, बल्कि अधिक विनाशकारी भी बन रही हैं। पहले बाढ़ केवल नदी या समुद्र के किनारे बसे क्षेत्रों तक सीमित थी, परंतु अब तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, गुरुग्राम, जयपुर, बेंगलूरु जैसे बड़े महानगर भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। यह न केवल एक जल-आपदा है, बल्कि यह शहर की समग्र व्यवस्था, नागरिकों की दिनचर्या, आधारभूत संरचनाओं और प्रशासनिक तंत्र पर भी गंभीर प्रभाव डालती है। जब कोई शहर बाढ़ की चपेट में आता है, तो उसकी संपूर्ण जीवनशैली, शहरी कार्यप्रणाली और प्रणालीगत ढांचा चरमराने लगता है।
आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव पड़ता है। दिहाड़ी मजदूर,रेहड़ी-पटरी वाले, छोटे दुकानदारों की आमदनी रुक जाती है। इससे उनकी आजीविका पर प्रभाव पड़ता है। उद्योगों, फैक्ट्रियों और दुकानों को बंद करना पड़ता है। व्यापार ठप हो जाते है, दुकानें बंद, गोदाम जलमग्न, कच्चा माल बर्बाद हो जाता है। बीमा कंपनियों और सरकारी तंत्र पर आर्थिक भार बढ़ता है।
घरों में पानी भरने से फर्नीचर, उपकरण, दस्तावेज और कपड़े बर्बाद हो जाते हैं जिससे आवास और संपत्ति पर प्रभाव पड़ता है। कच्चे मकान ढह जाते हैं, लोग बेघर हो जाते हैं। पुनर्निर्माण और मरम्मत में महीनों लग जाते हैं व आर्थिक बोझ बढ़ता है। बाढ़ के दौरान लोग अपने परिवार से बिछुड़ जाते हैं या सामूहिक आश्रय स्थलों पर रहने को मजबूर हो जाते हैं, जिससे उन पर मानसिक प्रभाव पड़ता है। सुरक्षा और निजता का संकट खड़ा हो जाता है, विशेषकर वयस्क महिलाओं और बच्चों के लिए। बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है क्योंकि स्कूलों में पानी भर जाता है या उन्हें राहत शिविरों में बदल दिया जाता है।
बाजारों में सब्जियां और आवश्यक वस्तएं महंगी हो जाती हैं क्योंकि आपूर्ति बाधित होती है, जिससे खाद्य और पेयजल संकट पैदा हो जाता है। पेयजल की उपलब्धता सीमित हो जाती है और लोग गंदा पानी पीने को विवश हो जाते हैं।
बच्चों, बुजुर्गों और विकलांगों की प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण वे जल्दी बीमार पड़ते हैं। इनके लिए जलभराव में चलना-फिरना लगभग असंभव हो जाता है। राहत शिविरों में सुविधाओं की कमी से इन वर्गों को विशेष रूप से कठिनाई होती है। महिलाओं को सुरक्षित शौचालय और स्नानगृह न मिलने की समस्या होती है। स्वच्छता उत्पादों की कमी से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। घरेलू जिम्मेदारियां और परिवार की देखभाल का बोझ और बढ़ जाता है। एम्बुलेंस और दमकल गाडिय़ों की आवाजाही बाधित हो जाती है, जिससे आपात सेवाओं पर प्रभाव पड़ता है। समय पर चिकित्सा सेवाएं न मिल पाने से गंभीर बीमारियों और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता है। जलजनित रोगों का प्रकोप जैसे हैजा, डेंगू, मलेरिया, त्वचा रोग, टायफाइड जैसे रोगों में वृद्धि होती है। चिकित्सा सेवाएं बाधित होती हैं। औषधियों और चिकित्सा उपकरणों की कमी हो जाती है । विशेषकर राहत शिविरों पर भी प्रभाव पड़ता है ।
बेघर हुए लोगों को पुनर्वास और रोजगार दिलवाना सरकार के लिए चुनौती बन जाता है, जिससे लोगों व उनके परिवार पर दीर्घकालिन प्रभाव पड़ता है। कई लोग स्थायी रूप से विस्थापित हो जाते हैं और गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं जिससे समाज में असमानता के साथ असुरक्षा की भावना बढ़ती है।
बाढ़ का बुनियादी ढांचे पर प्रभाव पड़ता है स्टोरों और गोदामों में पानी भरने से खाद्य सामग्री नष्ट हो जाती है। जल दबाव से सडक़ें उखड़ जाती हैं, गड्ढे बन जाते हैं, पुलों पर दरारें आ जाती हैं। सीवेज प्रणाली जाम हो जाती है, जिससे मल-मूत्र मिश्रित पानी सडक़ों पर बहता है जो दुर्गंध और संक्रमण फैलता है। पानी की टंकियां, पंप और पाइप लाइनें टूट जाती हैं, जिससे पीने योग्य जल की आपूर्ति रुक जाती है।
शहरी प्रशासन, नगर निकायों की प्रणाली पर प्रभाव व दबाव बढ़ जाते हैं। सीमित संसाधनों में अधिक क्षेत्रों की सफाई और राहत के कार्यों पर अधिकारियों को 24 घंटे सक्रिय रहना पड़ता है, जिससे प्रशासनिक योजना लडख़ड़ा जाती है। पुलिस और आपात सेवाएं भी प्रभावित होती हैं, जिससे राजनीतिक दबाव और जनता का आक्रोश के साथ नागरिक विरोध, आंदोलन और मीडिया में प्रशासनिक आलोचना बढ़ती है।
जल स्रोतों जैसे तालाब, झील और नाले दूषित हो जाते हैं। जैव विविधता पर असर पड़ता है, जिससे मछलियां, पक्षी और जलीय जीव मर जाते हैं इससे पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ता है। कचरे का बेतरतीब फैलाव और गंदगी का अंबार होने से कई समस्याएं पैदा हो जाती है। भूजल स्तर में असामान्यता भी नजर आने लगती है।
शहरी बाढ़ एक आपातकालीन परिस्थिति होती है। ऐसे संकट के समय नगर प्रशासन और सरकारी अधिकारियों की त्वरित, समन्वित और प्रभावशाली प्रतिक्रिया ही जनजीवन को सुरक्षित रखने में निर्णायक भूमिका निभाती है। यह न केवल जन-धन की रक्षा करता है, बल्कि प्रशासन के प्रति जनता का विश्वास भी बनाए रखता है। शहरी बाढ़ के दौरान प्रशासन को त्वरित कदम उठाने पड़ते है । यदि नगर प्रशासन और सरकारी अधिकारी त्वरित, समन्वित और मानवीय संवेदना से कार्य करें, तो इसके प्रभाव को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। यह सिर्फ एक प्रशासनिक चुनौती नहीं, बल्कि जन सेवा और कर्तव्यनिष्ठा की परीक्षा होती है। आपदा के समय उठाए गए तत्काल कदमों से ही जनता का विश्वास बनता है, जन-धन की रक्षा होती है, और एक शहर फिर से सामान्य जीवन की ओर लौट सकता है।
प्रशासन पूर्व-सतर्कता और तैयारी के तहत जलवायु पूर्वानुमान की निगरानी रखता है। मौसम विभाग और अन्य एजेंसियों के अलर्ट को नियमित रूप से मॉनिटर करना पड़ता है व संवेदनशील क्षेत्रों की सूची बनाकर निगरानी टीमों की तैनाती करता है। मोबाइल मैसेज, रेडियो, टीवी, वाट्सऐप और स्थानीय घोषणाओं के माध्यम से जनता को जानकारी देता है। बाढ़ संभावित क्षेत्रों के नागरिकों को घर खाली करने की सलाह भी देता है।
आपदा प्रबंधन योजना को सक्रिय करना होता है, जिसमें राज्य और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की टीमों को तत्पर रखना पड़ता है व फायर ब्रिगेड, पुलिस, होमगार्ड, मेडिकल टीम और गैर सरकारी संगठनों को अलर्ट मोड में लाना होता है।
राहत और बचाव कार्य के लिए जलभराव वाले क्षेत्रों में नावों और राफ्ट की व्यवस्था करानी होती है। लाइफ जैकेट, रस्सियां और ड्रोन कैमरों का प्रयोग करना है। राहत शिविरों की त्वरित स्थापना करना व सुरक्षित स्थानों पर भोजन, शौचालय, स्वच्छ पेयजल, दवाएं और बिस्तर की व्यवस्था करानी व महिलाओं, बच्चों, बुज़ुर्गों और विकलांगों के लिए अलग व्यवस्था साथ ही बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में मुफ्त मेडिकल कैंप, ओआरएस, टीकाकरण और सफाई अभियान चलाना व आधारभूत सेवाओं की बहाली जरूरी है, जिसमें बिजली और जल आपूर्ति की शीघ्र मरम्मत करना, डूबे हुए ट्रांसफार्मर और मोटरों को समय रहते ठीक करना व क्लोरीनेशन द्वारा जल स्रोतों को शुद्ध करना होता है।
सडक़ों और यातायात के संचालन के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा वैकल्पिक मार्ग सुझाना और भारी वाहनों को रोकना। कीचड़ आदि हटाना, गड्ढों को भरना व मरम्मत करवाना और संकेतक लगवाना। कचरे और मरे हुए जानवरों की तत्काल सफाई करवाना व नगर निगम और सफाई कर्मियों द्वारा विशेष व्यवस्था करवाना होता है।
जनसंपर्क और सूचना प्रबंधन के साथ शिकायत दर्ज कराने और मदद मांगने के लिए हेल्पलाइन, टोल-फ्री नंबर, वॉट्सऐप सुविधा उपलब्ध करना, ट्विटर, फेसबुक और वेबसाइट पर अपडेट उपलब्ध करना है। मीडिया को सही जानकारी देना, अफवाहों पर नियंत्रण और जनता को मीडिया द्वारा वास्तविक स्थिति से अवगत कराना व प्रशासनिक अधिकारी जनता से संवाद करें और भरोसा दिलाएं व समन्वय और आदेश प्रणाली की गतिविधियों पर निगरानी और नियंत्रण किया जा सके, जिसमें नगर निगम, स्वास्थ्य, जलदाय, विद्युत, परिवहन, पुलिस, फायर ब्रिगेड और स्वच्छता विभाग के बीच त्वरित समन्वय हो। जब शहरों में भारी बारिश होती है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जो निम्न भूमि में स्थित होते हैं। इस स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा, सतर्कता और जागरूकता अत्यंत आवश्यक होती है। उचित सावधानी बरतने से जन-धन की हानि से बचा जा सकता है। यदि नागरिक सतर्क, संयमित और जिम्मेदार रहें तो उनका असर कम किया जा सकता है। प्रशासन के साथ सहयोग करते हुए अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश अपनाना नितांत आवश्यक है। आपकी सतर्कता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
शहरी बाढ़ आधुनिक शहरों की एक गंभीर समस्या बन चुकी है। तेजी से होते शहरीकरण, असंतुलित विकास और जलवायु परिवर्तन के चलते बाढ़ की घटनाएं न केवल आम होती जा रही हैं, बल्कि अधिक विनाशकारी भी बन रही हैं। पहले बाढ़ केवल नदी या समुद्र के किनारे बसे क्षेत्रों तक सीमित थी, परंतु अब तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, गुरुग्राम, जयपुर, बेंगलूरु जैसे बड़े महानगर भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। यह न केवल एक जल-आपदा है, बल्कि यह शहर की समग्र व्यवस्था, नागरिकों की दिनचर्या, आधारभूत संरचनाओं और प्रशासनिक तंत्र पर भी गंभीर प्रभाव डालती है। जब कोई शहर बाढ़ की चपेट में आता है, तो उसकी संपूर्ण जीवनशैली, शहरी कार्यप्रणाली और प्रणालीगत ढांचा चरमराने लगता है।
आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव पड़ता है। दिहाड़ी मजदूर,रेहड़ी-पटरी वाले, छोटे दुकानदारों की आमदनी रुक जाती है। इससे उनकी आजीविका पर प्रभाव पड़ता है। उद्योगों, फैक्ट्रियों और दुकानों को बंद करना पड़ता है। व्यापार ठप हो जाते है, दुकानें बंद, गोदाम जलमग्न, कच्चा माल बर्बाद हो जाता है। बीमा कंपनियों और सरकारी तंत्र पर आर्थिक भार बढ़ता है।
घरों में पानी भरने से फर्नीचर, उपकरण, दस्तावेज और कपड़े बर्बाद हो जाते हैं जिससे आवास और संपत्ति पर प्रभाव पड़ता है। कच्चे मकान ढह जाते हैं, लोग बेघर हो जाते हैं। पुनर्निर्माण और मरम्मत में महीनों लग जाते हैं व आर्थिक बोझ बढ़ता है। बाढ़ के दौरान लोग अपने परिवार से बिछुड़ जाते हैं या सामूहिक आश्रय स्थलों पर रहने को मजबूर हो जाते हैं, जिससे उन पर मानसिक प्रभाव पड़ता है। सुरक्षा और निजता का संकट खड़ा हो जाता है, विशेषकर वयस्क महिलाओं और बच्चों के लिए। बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है क्योंकि स्कूलों में पानी भर जाता है या उन्हें राहत शिविरों में बदल दिया जाता है।
बाजारों में सब्जियां और आवश्यक वस्तएं महंगी हो जाती हैं क्योंकि आपूर्ति बाधित होती है, जिससे खाद्य और पेयजल संकट पैदा हो जाता है। पेयजल की उपलब्धता सीमित हो जाती है और लोग गंदा पानी पीने को विवश हो जाते हैं।
बच्चों, बुजुर्गों और विकलांगों की प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण वे जल्दी बीमार पड़ते हैं। इनके लिए जलभराव में चलना-फिरना लगभग असंभव हो जाता है। राहत शिविरों में सुविधाओं की कमी से इन वर्गों को विशेष रूप से कठिनाई होती है। महिलाओं को सुरक्षित शौचालय और स्नानगृह न मिलने की समस्या होती है। स्वच्छता उत्पादों की कमी से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। घरेलू जिम्मेदारियां और परिवार की देखभाल का बोझ और बढ़ जाता है। एम्बुलेंस और दमकल गाडिय़ों की आवाजाही बाधित हो जाती है, जिससे आपात सेवाओं पर प्रभाव पड़ता है। समय पर चिकित्सा सेवाएं न मिल पाने से गंभीर बीमारियों और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता है। जलजनित रोगों का प्रकोप जैसे हैजा, डेंगू, मलेरिया, त्वचा रोग, टायफाइड जैसे रोगों में वृद्धि होती है। चिकित्सा सेवाएं बाधित होती हैं। औषधियों और चिकित्सा उपकरणों की कमी हो जाती है । विशेषकर राहत शिविरों पर भी प्रभाव पड़ता है ।
बेघर हुए लोगों को पुनर्वास और रोजगार दिलवाना सरकार के लिए चुनौती बन जाता है, जिससे लोगों व उनके परिवार पर दीर्घकालिन प्रभाव पड़ता है। कई लोग स्थायी रूप से विस्थापित हो जाते हैं और गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं जिससे समाज में असमानता के साथ असुरक्षा की भावना बढ़ती है।
बाढ़ का बुनियादी ढांचे पर प्रभाव पड़ता है स्टोरों और गोदामों में पानी भरने से खाद्य सामग्री नष्ट हो जाती है। जल दबाव से सडक़ें उखड़ जाती हैं, गड्ढे बन जाते हैं, पुलों पर दरारें आ जाती हैं। सीवेज प्रणाली जाम हो जाती है, जिससे मल-मूत्र मिश्रित पानी सडक़ों पर बहता है जो दुर्गंध और संक्रमण फैलता है। पानी की टंकियां, पंप और पाइप लाइनें टूट जाती हैं, जिससे पीने योग्य जल की आपूर्ति रुक जाती है।
शहरी प्रशासन, नगर निकायों की प्रणाली पर प्रभाव व दबाव बढ़ जाते हैं। सीमित संसाधनों में अधिक क्षेत्रों की सफाई और राहत के कार्यों पर अधिकारियों को 24 घंटे सक्रिय रहना पड़ता है, जिससे प्रशासनिक योजना लडख़ड़ा जाती है। पुलिस और आपात सेवाएं भी प्रभावित होती हैं, जिससे राजनीतिक दबाव और जनता का आक्रोश के साथ नागरिक विरोध, आंदोलन और मीडिया में प्रशासनिक आलोचना बढ़ती है।
जल स्रोतों जैसे तालाब, झील और नाले दूषित हो जाते हैं। जैव विविधता पर असर पड़ता है, जिससे मछलियां, पक्षी और जलीय जीव मर जाते हैं इससे पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ता है। कचरे का बेतरतीब फैलाव और गंदगी का अंबार होने से कई समस्याएं पैदा हो जाती है। भूजल स्तर में असामान्यता भी नजर आने लगती है।
शहरी बाढ़ एक आपातकालीन परिस्थिति होती है। ऐसे संकट के समय नगर प्रशासन और सरकारी अधिकारियों की त्वरित, समन्वित और प्रभावशाली प्रतिक्रिया ही जनजीवन को सुरक्षित रखने में निर्णायक भूमिका निभाती है। यह न केवल जन-धन की रक्षा करता है, बल्कि प्रशासन के प्रति जनता का विश्वास भी बनाए रखता है। शहरी बाढ़ के दौरान प्रशासन को त्वरित कदम उठाने पड़ते है । यदि नगर प्रशासन और सरकारी अधिकारी त्वरित, समन्वित और मानवीय संवेदना से कार्य करें, तो इसके प्रभाव को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। यह सिर्फ एक प्रशासनिक चुनौती नहीं, बल्कि जन सेवा और कर्तव्यनिष्ठा की परीक्षा होती है। आपदा के समय उठाए गए तत्काल कदमों से ही जनता का विश्वास बनता है, जन-धन की रक्षा होती है, और एक शहर फिर से सामान्य जीवन की ओर लौट सकता है।
प्रशासन पूर्व-सतर्कता और तैयारी के तहत जलवायु पूर्वानुमान की निगरानी रखता है। मौसम विभाग और अन्य एजेंसियों के अलर्ट को नियमित रूप से मॉनिटर करना पड़ता है व संवेदनशील क्षेत्रों की सूची बनाकर निगरानी टीमों की तैनाती करता है। मोबाइल मैसेज, रेडियो, टीवी, वाट्सऐप और स्थानीय घोषणाओं के माध्यम से जनता को जानकारी देता है। बाढ़ संभावित क्षेत्रों के नागरिकों को घर खाली करने की सलाह भी देता है।
आपदा प्रबंधन योजना को सक्रिय करना होता है, जिसमें राज्य और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की टीमों को तत्पर रखना पड़ता है व फायर ब्रिगेड, पुलिस, होमगार्ड, मेडिकल टीम और गैर सरकारी संगठनों को अलर्ट मोड में लाना होता है।
राहत और बचाव कार्य के लिए जलभराव वाले क्षेत्रों में नावों और राफ्ट की व्यवस्था करानी होती है। लाइफ जैकेट, रस्सियां और ड्रोन कैमरों का प्रयोग करना है। राहत शिविरों की त्वरित स्थापना करना व सुरक्षित स्थानों पर भोजन, शौचालय, स्वच्छ पेयजल, दवाएं और बिस्तर की व्यवस्था करानी व महिलाओं, बच्चों, बुज़ुर्गों और विकलांगों के लिए अलग व्यवस्था साथ ही बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में मुफ्त मेडिकल कैंप, ओआरएस, टीकाकरण और सफाई अभियान चलाना व आधारभूत सेवाओं की बहाली जरूरी है, जिसमें बिजली और जल आपूर्ति की शीघ्र मरम्मत करना, डूबे हुए ट्रांसफार्मर और मोटरों को समय रहते ठीक करना व क्लोरीनेशन द्वारा जल स्रोतों को शुद्ध करना होता है।
सडक़ों और यातायात के संचालन के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा वैकल्पिक मार्ग सुझाना और भारी वाहनों को रोकना। कीचड़ आदि हटाना, गड्ढों को भरना व मरम्मत करवाना और संकेतक लगवाना। कचरे और मरे हुए जानवरों की तत्काल सफाई करवाना व नगर निगम और सफाई कर्मियों द्वारा विशेष व्यवस्था करवाना होता है।
जनसंपर्क और सूचना प्रबंधन के साथ शिकायत दर्ज कराने और मदद मांगने के लिए हेल्पलाइन, टोल-फ्री नंबर, वॉट्सऐप सुविधा उपलब्ध करना, ट्विटर, फेसबुक और वेबसाइट पर अपडेट उपलब्ध करना है। मीडिया को सही जानकारी देना, अफवाहों पर नियंत्रण और जनता को मीडिया द्वारा वास्तविक स्थिति से अवगत कराना व प्रशासनिक अधिकारी जनता से संवाद करें और भरोसा दिलाएं व समन्वय और आदेश प्रणाली की गतिविधियों पर निगरानी और नियंत्रण किया जा सके, जिसमें नगर निगम, स्वास्थ्य, जलदाय, विद्युत, परिवहन, पुलिस, फायर ब्रिगेड और स्वच्छता विभाग के बीच त्वरित समन्वय हो। जब शहरों में भारी बारिश होती है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जो निम्न भूमि में स्थित होते हैं। इस स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा, सतर्कता और जागरूकता अत्यंत आवश्यक होती है। उचित सावधानी बरतने से जन-धन की हानि से बचा जा सकता है। यदि नागरिक सतर्क, संयमित और जिम्मेदार रहें तो उनका असर कम किया जा सकता है। प्रशासन के साथ सहयोग करते हुए अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश अपनाना नितांत आवश्यक है। आपकी सतर्कता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
संबंधित खबरें
Hindi News / Opinion / जलभराव के दौरान सतर्कता ही सबसे बड़ी सुरक्षा
Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.