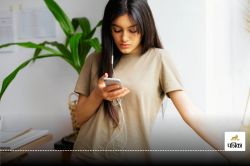अग्निर्जागार तमृच: कामयन्ते-अग्निर्जागर-तमु सामानि यन्ति। अग्निर्जागार-तमयं सोम आह-तवाहमस्मि सख्ये न्योका:।। अग्नि व सोम ही स्थूल शरीर में क्रमश: पुरुष और स्त्री है। पुरुष में आग्नेय और स्त्री में सौम्य भाव की प्रबलता रहती है। किन्तु पुरुष व स्त्री दोनों में क्रमश: सोम व अग्नि भी रहता है क्योंकि याज्ञिक सृष्टि में दोनों के मेल से ही सृजन होता है। यही कारण है कि सृष्टि को अग्निषोमात्मकम् कहा जाता है।
पुरुष भीतर सोम है, बाहर अग्नि है। इसके विपरीत स्त्री भीतर अग्नि है, बाहर सोम है। अर्थात् आपसी व्यवहार में ये दो नहीं हैं, चार हैं। सतही व्यवहार में दो हैं, निजी व्यवहार में चार हैं। क्षणिक व्यवहार अल्पकालीन होता है। इसका भीतर अंकन नहीं होता। व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं करता। अग्नि व सोम की घन-तरल-विरल अवस्थाओं के आधार पर स्त्री-पुरुष का आदान-प्रदान छह-छह स्तर का हो जाता है। पुरुष के बाहरी अग्नि के तीन स्तर, भीतर सोम के तीन स्तर। स्त्री के बाहरी सौम्यता के तीन स्तर, भीतर आग्नेयता तीन स्तर। यद्यपि सारे स्तर साधन मात्र हैं क्योंकि कर्म की दिशा मन से होती है। मन की क्या कामना है। उसमें विद्या भाव प्रधान है, अथवा अविद्या भाव प्रधान है। मन में कामना मात्र ही है, अथवा उसे कर्म रूप भी देना है। एक स्थिति यह भी हो सकती है कि कामना ईश्वर/प्रकृति की है या जीवात्मा की- नए कर्म की।
स्वभाव-प्रकृति के आकलन का मार्ग भी यही है। इसमें स्थायी सम्बन्ध, अस्थायी व्यवहार तथा निजी ऋण मुक्ति के कारण आदान-प्रदान सभी दिखाई पड़ते हैं। व्यवहार का स्तर स्थूल मन है, सूक्ष्म मन है अथवा कारण शरीर का मन। वैसा ही स्तर और दिशा का अर्थ समझ में आ जाएगा। समय के साथ सभ्यता इतनी बदल गई कि संस्कृति धराशायी होने लगी, सूक्ष्म और कारण गौण हो गए। केवल स्थूल रह गया। जबकि पुरुष का सौम्यता का क्षेत्र और स्त्री का आग्नेय क्षेत्र दोनों सूक्ष्म हैं। भीतर जाकर ही और जीकर ही समझे जा सकते हैं। दोनों के ही भीतरी स्वरूप जीवन से लगभग बाहर ही निकल गए हैं।
पुरुष आज सोमगर्भित अग्नि प्रधान नहीं रह गया। मात्र आग्नेय घन है। संस्कार से कुछ पुरुष तरल-विरल हो सकते हैं। नई पीढ़ी का पुरुष एकांगी अग्नि पिण्ड बनता जा रहा है। सोम अग्नि का पोषक तत्त्व है। इसके अभाव में एक सीमा पर पहुंच कर अग्नि स्वयं भस्मीभूत हो जाता है। अति विकसित, अतिशिक्षित देशों के पुरुष इस मार्ग को चुन चुके। आज की स्त्री भी उनकी भांति ही विकसित होना जीवन की सार्थकता मानती है। वह भी अग्निगर्भित सौम्यमूर्ति बने रहने की इच्छुक नहीं है। उसे अपने स्त्रैण स्वरूप तथा सूक्ष्म प्रकृति को समझकर उसका अनुसरण करने की आवश्यकता ही नहीं लगती। वह भी पुरुष के समकक्ष होकर अपना पौरुष पुष्ट करना चाहती है। सौम्यता उसकी प्राथमिकता न रहकर पौरुष के भेंट चढ़ती जा रही है। शरीर के बारे में वह भी पुरुष की तरह स्वच्छन्द रहना चाह रही है। बुद्धि से भी वह पुरुष से आगे रहने के प्रयास में है। उसके स्त्रैण पक्ष का स्थान उष्णता-अहंकार-आक्रामकता लेते जा रहे हैं। वह भीतर से संकल्पित होकर अग्नि को पुष्ट करने में जुट गई है। स्वयं को पुरुष से अलग करके दिखाई देने को आतुर है। अपने पौरुष और बुद्धिबल के आधार पर।
जैसे-जैसे स्त्री अपने पौरुष का पोषण बढ़ाएगी, उसके सोम का क्षरण बढ़ता जाएगा। मूलत: उसका सोम ही अग्नि में आहुत होकर आग्नेय हो जाएगा। वह स्वयं को पुरुष मानकर ही व्यवहार करने लगेगी। उसका पत्नी स्वरूप भी पौरुषेय होने लगेगा। आकर्षण तो गया। यही स्वरूप विच्छेद के मार्ग को प्रशस्त करता है। अग्नि को तरलता एवं विरलता देना सहज नहीं है। अग्नि विशकलन करता है, तोड़ता है। उसको स्नेह प्रज्वलित ही करता है।
पुरुष के साथ विपरीत भाव दिखाई देता है। उसका अग्नि ऊपर ही उठ सकता है, नीचे प्रवाहित नहीं होता। सोम अधोगति प्राप्त करता है। अत: स्त्री सहजता से कठोर हो सकती है। पुरुष का सोम निर्बल भी है और अधोगामी भी होता है। जीवन में उसकी दिशा बदल पाना कठिन है। अग्नि भी घन है, बुद्धि से भी उष्ण है। अत: उसका अहंकार अधिक प्रभावी रहता है। यदि भाव भी नकारात्मक हो जाए तो स्वभाव से आसुरी हो जाएगा।
आग्नेय पुरुष में माधुर्य, विनम्रता, भक्ति का अभाव ही रहता है। ये गुण तो पुष्ट मन के हैं। जहां ‘स्व’ का अभाव है, वहां मातृत्व है। अग्नि सदा अभाव ग्रस्त होता है। उसे नियमित खुराक (पोषण) की आवश्यकता रहती है। अन्न का अभाव ही उसे रौद्र तक बना देता है। सोम में यह अभाव नहीं होता। वह अग्नि के अभाव का पूरक होता है। यही निर्माण का प्राकृतिक सिद्धान्त भी है।
सोम का घनरूप पानी है। पानी अग्निशमन का कार्य करता है। स्त्री के श्रद्धा, वात्सल्य, स्नेह जैसे भाव ठोस रहते हैं, तो पुरुष का अग्नि उग्र न होकर तरल और विरल होने लगता है। दाम्पत्य भाव की यही पूर्णता स्वर्ग का सुख देती है। स्त्री की घनात्मक सौम्यता ही उसकी दिव्यता है। उसके जन्म और पोषण के कार्यों का आधार है। पुरुष के लिए इस स्तर तक सौम्य हो जाना दुरूह कार्य है। भक्ति ही शायद ऐसा मार्ग है। पुरुष का अहंकार झुकने और समर्पण करने को तैयार होता ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि
‘‘शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान।’’ भक्ति गुरु का मार्ग है। विद्यार्जन का, ज्ञान का मार्ग है। गुरु के सान्निध्य में ही अग्नि तरल और विरल हो सकता है। अग्नि ही विरलता की चरम अवस्था में सोम बन जाता है। पुरुष के सारे पुरुषार्थ यहां समाप्त हो जाते हैं। पुरुष पूर्ण सौम्य होकर अपने महापुरुष में लीन होने को तैयार है। यही मोक्ष है।
क्रमश: gulabkothari@epatrika.com