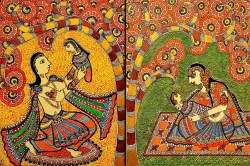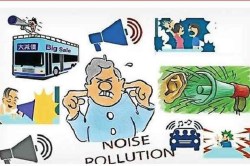Sunday, April 13, 2025
भगवान महावीर : भारतीय आध्यात्मिक आकाश के ध्रुव तारे
– जसबीर सिंह ( पूर्व अध्यक्ष, राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग )
जयपुर•Apr 10, 2025 / 12:33 pm•
विकास माथुर
भगवान महावीर ने अपने पूरे जीवन काल में न व्यर्थ बोला, न व्यर्थ सोचा, न व्यर्थ किया। उनके जीवन में एक मर्यादा थी। वे भारतीय आध्यात्मिक आकाश के ध्रुव तारे हैं। वे एक अध्यात्म-पुरुष तो थे ही लेकिन उनके व्यक्ति के संदर्भ में दिए गए संदेशों के स्वभावत: सामाजिक आयाम भी स्थापित हुए। उनके संदेशों के महत्त्व व प्रासांगिकता में समाज का हित भी समाहित है।
संबंधित खबरें
जैन परम्परा का आदर्श वाक्य ‘परस्परोग्रहो जीवानाम्’ है जो इस बात को इंगित करता है कि पारस्परिकता एक सभ्य व सुसंस्कृत समाज की आधारशिला है और इसे पल्लवित किया जाना चाहिए। भगवान महावीर का जीवन, आचरण व संदेश जहां आध्यात्मिक पराकाष्ठा है, वहीं उनमें समाज के लिए उपयोगी संदेश भी छिपे हुए हैं। शताब्दियों से भारतीय समाज में ऊंच-नीच का भेदभाव बहुत बड़ी समस्या रही। भगवान महावीर ने इस पर प्रहार करते हुए स्पष्टत: कहा कि न कोई छोटा है न बड़ा। अनेक लोग प्रश्न करते हैं कि जब इस संसार में कोई बलवान है कोई निर्बल, कोई बुद्धिमान कोई कम समझ, कोई धनवान कोई निर्धन तो कैसे कहा जा सकता है कि छोटे व बड़े का कोई भेद नहीं है। भगवान महावीर का कहना है कि व्यक्ति आत्मा है, वह शरीर, मन या बुद्धि नहीं है। यह विषमता आगंतुक है, आत्मगत नहीं। अत: इसे महत्त्व नहीं देना चाहिए। उन्होंने व्यक्तियों की आत्मगत समानता को महत्त्व दिया जिससे श्रेष्ठता अथवा हीनता की ग्रंथियां बनने की बजाय सबका एक दूसरे के प्रति सद्भाव व सौहार्द का भाव बने। जातिवाद की दार्शनिक व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि मनुष्य मात्र की एक जाति है।
बंधुत्व की भावना समाज की रीढ़ है और बंधुत्व का अभाव समाज को मात्र भीड़ में बदल देगा। उन्होंने जैन परम्परा के त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र को समझाया। साथ ही अहिंसा, अपरिग्रह, अकाम, अचौर्य व अप्रमाद के अति बहुमूल्य सिद्धांत हमें दिए जो सदियों से हमारे प्रेरणासूत्र बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि हिंसा, परिग्रह, काम, चौर्य व प्रमाद मनुष्य के स्वभाव हैं। साधना, तपस्या, संयम व चिंतन से ही इन स्वभावों को अहिंसा, अपरिग्रह, अकाम, अचौर्य व अप्रमाद की सिद्धियों व विधियों में बदला जा सकता है। उन्होंने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए होशपूर्वक जीने (अप्रमाद) को बहुत महत्त्व दिया। उनके पास जब एक नौजवान पूछने गया कि मैं क्या करूं जिससे मेरा जीवन सफल हो जाए तो उन्होंने उसे कहा कि यह चिंता छोड़ो कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तुम जो भी करते हो उसे होशपूर्वक करो। जब तुम प्रत्येक कृत्य को होशपूर्वक यानी अप्रमाद में करोगे तो वही करने लग जाओगे जो करने योग्य है। अगर तुम क्रोध भी होशपूर्वक करोगे तो क्रोध हमेशा के लिए तुम्हारे जीवन से विदा हो जाएगा।
शिष्य गौतम ने एक बार उनसे पूछा कि मुनि कौन है तो उन्होंने संक्षिप्त किंतु अनूठा उत्तर दिया कि ‘असुप्ता मुनि’। गौतम ने पूछा कि फिर अमुनि कौन है तो उत्तर फिर संक्षिप्त किंतु अनोखा था ‘सुप्ता अमुनि’। उनके कहने का अर्थ था कि बेहोशी में जीया हुआ जीवन व्यर्थ है और ऐसा जीवन मूल्यहीन है। प्रमाद किया तो जागरूकता विदा हो गई और जागरूकता गई तो राग-द्वेष आक्रमण कर देंगे। अप्रमाद सांसारिक व्यक्तियों के लिए भी बहुत उपयोगी है। प्रमादी व्यक्ति को लौकिक क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। अप्रमाद का व्यापक अर्थ है पूर्ण मनोयोग व जागरूकता से किसी कार्य को करना। ऐसा अप्रमाद व जागरूकता सांसारिक सफलता के लिए भी अचूक दवा या मंत्र है।
भगवान महावीर का अंहिसा का संदेश इस जगत को उनका अमूल्य उपहार है। अहिंसा का अर्थ समझा जाता है कि किसी को कष्ट न दिया जाए। यह अर्थ गलत भी नहीं है, लेकिन भगवान महावीर ने अहिंसा को इतने से स्थूल रूप में नहीं कहा। उन्होंने कहा कि राग-द्वेष का न होना ही अहिंसा है। अहिंसक होने का अहंकार होना भी हिंसा है। उन्होंने जहां अहिंसा पर इतना जोर दिया, वहीं विनम्रता के गुण को भी आदर्श जीवन के लिए अति आवश्यक बताया। इसलिए जैन परम्परा में आठ प्रकार के अहंकार भी त्याज्य बताए गए हैं। ये हैं अपनी बुद्धि का अहंकार, अपनी धार्मिकता का अहंकार, अपने वंश का अहंकार, अपनी जाति का अहंकार, अपने शरीर या मनोबल का अहंकार, अपनी चमत्कार दिखाने वाली शक्तियों का अहंकार, योग और तपस्या का अहंकार तथा रूप और सौंदर्य का अहंकार। इतनी तैयारी होने पर ही भगवान महावीर के अनुसार सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र का फल व्यक्ति को मिल सकता है।
भगवान महावीर ने व्यक्ति को श्रेष्ठ बनने के लिए अणुव्रत का नियम दिया। जिस तरह छोटे-छोटे अणुओं द्वारा बने अणुबम से प्रचंड विस्फोट हो सकता है, वैसे ही छोटे-छोटे व्रतों का पालन करके व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक व क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकते हैं। अणुव्रतों के पालन से सामाजिक व व्यक्तिगत दृष्टि से जो अनुचित है, इसका त्याग किया जा सकता है। इस प्रकार भगवान महावीर ने अणुव्रतों के माध्यम से एक स्वस्थ समाज के निर्माण की हमें आसान परिकल्पना व दृष्टि दी। उनके द्वारा दिया गया एक अन्य महत्त्वपूर्ण सिद्धांत वर्तमान संदर्भों में अनेकांत का है। उनके समय में भी समाज में अनेक सम्प्रदाय थे जो अपने अपने सिद्धांत, नियम व परम्पराएं रखते थे। उन्होंने घोषणा की कि कोई भी व्यक्ति सत्य के एक अंश या पक्ष को ही उद्घाटित कर सकता है, सम्पूर्ण सत्य को नहीं। यदि कोई सत्य के एक अंश को ही संपूर्ण सत्य मानकर अपने को सत्य और दूसरे को मिथ्या घोषित करेगा तो कलह व टकराहट निश्चित है। दुनिया का इतिहास गवाह है कि इसी कारण धर्म के नाम पर जितने युद्ध हुए हैं, अन्य किसी कारण से नहीं।
भारतीय समाज के लिए तो वर्तमान संदर्भ में अनेकांत का सिद्धान्त अतिश्रेष्ठ है क्योंकि हमारे समाज में तो कुछ कोस की दूरी पर ही बोलियां, लिपियां, रस्मों रिवाज, देवता व कुल देवता बदल जाते हैं। भारत जैसे देश के लिए तो कहा भी जाता है ‘चार कोस पर बदले पानी, आठ कोस पर वाणी।’ भगवान महावीर को अनेक कष्ट देने वाले मिले, उनके कानों में कीलें ठोकने वाले और पत्थर मारने वाले मिले, गांव से खदेड़ कर बाहर करने वाले भी मिले पर उन्होंने सदैव कहा ‘मित्ति में सव्व भूए सू, वैरं मज्झ न केवई’ अर्थात ‘मेरी मित्रता सबसे है, सारे विश्व से है और वैर मेरा किसी से भी नही।’ उनका कहना था कि शत्रुता से शत्रुता समाप्त नहीं होती, क्रोध से क्रोध समाप्त नहीं होता, वैर से वैर नहीं मिटता। जितना वैर बढ़ता जाता है, उतना तुम अपने चारों तरफ अपने ही हाथों से नरक निर्मित करते चले जाते हो।
Hindi News / Opinion / भगवान महावीर : भारतीय आध्यात्मिक आकाश के ध्रुव तारे
यह खबरें भी पढ़ें
लेटेस्ट ओपिनियन न्यूज़
Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.