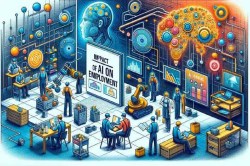Friday, May 2, 2025
डिजिटल दुनिया में सिमटता जा रहा बचपन
डॉ. शिवम भारद्वाज
जयपुर•May 01, 2025 / 05:40 pm•
Neeru Yadav
आज के बच्चों का बचपन एक विचित्र दौर और द्वंद्व से गुजर रहा है। एक ओर डिजिटल तकनीक ने बच्चों के सामने ज्ञान, वैश्विक संपर्क और रचनात्मकता के नए क्षितिज खोले हैं, वहीं दूसरी ओर यह तकनीक उनके विकास के नैसर्गिक आयामों को क्षीण करती प्रतीत हो रही है। वह मैदानों की माटी से कटकर स्क्रीन की चमक में उलझता जा रहा है। यह परिवर्तन केवल दृश्य स्तर पर नहीं, बल्कि सामाजिक, मानसिक और शारीरिक रूप से भी गहरे असर डाल रहा है।
कुछ दशक पहले तक बच्चों की दिनचर्या मे मोहल्लों की गलियों में भागदौड़ और खेल के मैदानों की एक खास जगह होती थी। गिल्ली-डंडा, खो-खो, पिट्ठू, कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल, दौड़, लुका-छिपी और कंचे जैसे खेल केवल मनोरंजन नहीं थे, बल्कि वे जीवन के प्राथमिक विद्यालय समान थे। कंचों की पंक्तियाँ बनाकर निशाना साधना हो या गिल्ली को हवा में मारना — यह केवल खेल नहीं बल्कि एकाग्रता, धैर्य और संतुलन का अभ्यास था। इन खेलों के माध्यम से बच्चे सामूहिकता, नेतृत्व, सहयोग और सहानुभूति जैसे गुणों को स्वाभाविक रूप से आत्मसात करते थे। मिट्टी से जुड़ाव और शारीरिक सक्रियता उनके मानसिक संतुलन और सामाजिक विकास के लिए आधारशिला का काम करते थे।
लेकिन 1990 के दशक के बाद भारत में इंटरनेट और मोबाइल तकनीक का जिस तीव्र गति से प्रसार हुआ, उसने बच्चों की दिनचर्या, प्राथमिकताएं और सामाजिकता को ही बदल दिया। आज के बच्चे मैदानों से कटकर स्क्रीन तक सीमित हो गए हैं। क्रिकेट का बल्ला अब हाथ में नहीं, उँगलियों की टैप में बदल गया है। दोस्तों के साथ दौड़ने-खेलने की जगह अब वीडियो गेम के आभासी पात्रों ने ले ली है।
आज की पीढ़ी उस उम्र में जब उसे दौड़ना, गिरना, खेलते हुए जीतना और हारना सीखना चाहिए था, वह घंटों एकाकी होकर स्क्रीन की ओर ताक रही है। मानसिक तनाव, आत्मिक अकेलापन और सामाजिक अलगाव जैसी स्थितियाँ तमाम बच्चों की वास्तविकता बनती जा रही हैं। तकनीक के इस अंध-आकर्षण ने बच्चों को एक आभासी प्रतिस्पर्धा में झोंक दिया है, जहाँ न भावनात्मक समझ है, न सामाजिक संवाद का अभ्यास।
पारंपरिक खेलों की विशेषता यही थी कि वे केवल शारीरिक क्रियाएँ नहीं थे, वे जीवन-दर्शन के शिक्षक थे। खो-खो में टीम के लिए दौड़ते हुए बच्चे सीखते थे सामूहिक प्रतिबद्धता; क्रिकेट में साझेदारी और रणनीति के भाव निखरते थे; फुटबॉल में तालमेल और लक्ष्य की ओर एकजुटता का अनुभव होता था; गिल्ली-डंडा और पिट्ठू जैसे खेलों में एकाग्रता, चपलता और संतुलन का सहज प्रशिक्षण मिलता था। ये सभी खेल बच्चों को भीतर से मज़बूत करते थे — भावनात्मक, शारीरिक-मानसिक और सामाजिक स्तर पर। शोध अध्ययनों के अनुसार बीते एक दशक में भारत में बच्चों के मोटापे में चिंताजनक वृद्धि हुई है और इसके प्राथमिक कारणों में शारीरिक गतिविधियों में कमी, अत्यधिक स्क्रीन समय और निष्क्रिय जीवनशैली भी प्रमुख रूप से सामने आए हैं। यह केवल शारीरिक स्वास्थ्य का नहीं, सामाजिक असंतुलन का भी संकेत है।
हालाँकि यह कहना अनुचित होगा कि यह सब तकनीक का दोष है। ऑनलाइन शिक्षा, कोडिंग, डिजिटल रचनात्मकता जैसे माध्यमों ने बच्चों को वैश्विक क्षितिज पर जोड़ा है। परंतु इस तकनीक का असंतुलित और अनियंत्रित ढंग से इस्तेमाल बच्चों को उनके शरीर, मन और समाज से काटने लगता है, और ऐसे में वह विकास का माध्यम काम, अवरोध का कारण ज्यादा बन जाती है।
ऐसे में यह बेहद आवश्यक हो जाता है कि हम तकनीक और परंपरा के बीच संतुलन स्थापित करें। यहाँ फिनलैंड जैसे देशों का मॉडल प्रेरणादायक है, जहाँ डिजिटल शिक्षा के साथ-साथ प्रकृति-आधारित गतिविधियाँ, आउटडोर खेल और सहयोगात्मक शिक्षण को समान प्राथमिकता दी जाती है। भारत में ‘फिट इंडिया मूवमेंट’ और ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020’ जैसे प्रयास इस दिशा में आशाजनक शुरुआत हैं, लेकिन इनका प्रभाव तभी होगा जब इन्हें विद्यालयों, समुदायों और परिवारों तक ठोस रूप में पहुँचाया जाए।
विद्यालयों में पारंपरिक खेलों को पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग बनाना, खेल मैदानों का पुनरुद्धार, और अभिभावकों द्वारा अपने बच्चों के स्क्रीन समय का विवेकपूर्ण नियंत्रण — ये कुछ ऐसे ठोस कदम हैं जो बच्चों को दोबारा संतुलित और सक्रिय बचपन की ओर ले जा सकते हैं। साथ ही, शिक्षा में भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सामाजिक संवाद कौशल को स्थान देना भी समय की आवश्यकता बन चुका है।
बचपन की असली सुंदरता सिर्फ खेलों, या मस्ती के पलों में नहीं है, बल्कि उन क्षणों में है जब बच्चे अपने जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सीखते हैं। वे खेल, मित्रता, प्रतिस्पर्धा और सामूहिकता के माध्यम से अपना व्यक्तित्व गढ़ते हैं, और यही उन्हें जीवन के संघर्षों से निपटने के लिए तैयार करता है। आज, जब तकनीकी दुनिया बच्चों को एकाकी बनाने की चुनौती सामने रख रही है, जब तमाम बच्चे इस आभासी दुनिया में खोये लगते हैं, तो सवाल वाजिब हैं कि क्या हम उस पुरानी खुशबू, उस मिट्टी की महक, उस गिल्ली-डंडे और कंचे के खेल को फिर से लौटा सकते हैं? क्या हम उस गली-मोहल्ले को फिर से जीवित कर सकते हैं, जहाँ बच्चों की हंसी और दौड़-भाग से सजीव था हर एक कोना?
एक देश का भविष्य उसके बच्चों में छुपा होता है। और जब वे अपनी मिट्टी से जुड़कर खेलते हैं, जब वे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, तो न केवल उनका, बल्कि पूरे समाज का भविष्य उज्जवल होता है। यही वह आधार है, जिस पर भारत का समृद्ध और समावेशी समाज खड़ा होगा। यह सामूहिक और साझा ज़िम्मेदारी है — सरकार, समाज और परिवार की — कि बच्चों को एक ऐसा संतुलित और समृद्ध बचपन दें, जहाँ वे तकनीक के साथ-साथ जीवन के वास्तविक पाठ भी सीखें। यदि हम इस संतुलन को साध पाए, तो हम न केवल एक स्वस्थ और सशक्त पीढ़ी तैयार करेंगे, बल्कि हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे, जो अपने मूल्यों, अपनी पहचान और अपनी शक्ति को समझने वाला हो।
कुछ दशक पहले तक बच्चों की दिनचर्या मे मोहल्लों की गलियों में भागदौड़ और खेल के मैदानों की एक खास जगह होती थी। गिल्ली-डंडा, खो-खो, पिट्ठू, कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल, दौड़, लुका-छिपी और कंचे जैसे खेल केवल मनोरंजन नहीं थे, बल्कि वे जीवन के प्राथमिक विद्यालय समान थे। कंचों की पंक्तियाँ बनाकर निशाना साधना हो या गिल्ली को हवा में मारना — यह केवल खेल नहीं बल्कि एकाग्रता, धैर्य और संतुलन का अभ्यास था। इन खेलों के माध्यम से बच्चे सामूहिकता, नेतृत्व, सहयोग और सहानुभूति जैसे गुणों को स्वाभाविक रूप से आत्मसात करते थे। मिट्टी से जुड़ाव और शारीरिक सक्रियता उनके मानसिक संतुलन और सामाजिक विकास के लिए आधारशिला का काम करते थे।
लेकिन 1990 के दशक के बाद भारत में इंटरनेट और मोबाइल तकनीक का जिस तीव्र गति से प्रसार हुआ, उसने बच्चों की दिनचर्या, प्राथमिकताएं और सामाजिकता को ही बदल दिया। आज के बच्चे मैदानों से कटकर स्क्रीन तक सीमित हो गए हैं। क्रिकेट का बल्ला अब हाथ में नहीं, उँगलियों की टैप में बदल गया है। दोस्तों के साथ दौड़ने-खेलने की जगह अब वीडियो गेम के आभासी पात्रों ने ले ली है।
आज की पीढ़ी उस उम्र में जब उसे दौड़ना, गिरना, खेलते हुए जीतना और हारना सीखना चाहिए था, वह घंटों एकाकी होकर स्क्रीन की ओर ताक रही है। मानसिक तनाव, आत्मिक अकेलापन और सामाजिक अलगाव जैसी स्थितियाँ तमाम बच्चों की वास्तविकता बनती जा रही हैं। तकनीक के इस अंध-आकर्षण ने बच्चों को एक आभासी प्रतिस्पर्धा में झोंक दिया है, जहाँ न भावनात्मक समझ है, न सामाजिक संवाद का अभ्यास।
पारंपरिक खेलों की विशेषता यही थी कि वे केवल शारीरिक क्रियाएँ नहीं थे, वे जीवन-दर्शन के शिक्षक थे। खो-खो में टीम के लिए दौड़ते हुए बच्चे सीखते थे सामूहिक प्रतिबद्धता; क्रिकेट में साझेदारी और रणनीति के भाव निखरते थे; फुटबॉल में तालमेल और लक्ष्य की ओर एकजुटता का अनुभव होता था; गिल्ली-डंडा और पिट्ठू जैसे खेलों में एकाग्रता, चपलता और संतुलन का सहज प्रशिक्षण मिलता था। ये सभी खेल बच्चों को भीतर से मज़बूत करते थे — भावनात्मक, शारीरिक-मानसिक और सामाजिक स्तर पर। शोध अध्ययनों के अनुसार बीते एक दशक में भारत में बच्चों के मोटापे में चिंताजनक वृद्धि हुई है और इसके प्राथमिक कारणों में शारीरिक गतिविधियों में कमी, अत्यधिक स्क्रीन समय और निष्क्रिय जीवनशैली भी प्रमुख रूप से सामने आए हैं। यह केवल शारीरिक स्वास्थ्य का नहीं, सामाजिक असंतुलन का भी संकेत है।
हालाँकि यह कहना अनुचित होगा कि यह सब तकनीक का दोष है। ऑनलाइन शिक्षा, कोडिंग, डिजिटल रचनात्मकता जैसे माध्यमों ने बच्चों को वैश्विक क्षितिज पर जोड़ा है। परंतु इस तकनीक का असंतुलित और अनियंत्रित ढंग से इस्तेमाल बच्चों को उनके शरीर, मन और समाज से काटने लगता है, और ऐसे में वह विकास का माध्यम काम, अवरोध का कारण ज्यादा बन जाती है।
ऐसे में यह बेहद आवश्यक हो जाता है कि हम तकनीक और परंपरा के बीच संतुलन स्थापित करें। यहाँ फिनलैंड जैसे देशों का मॉडल प्रेरणादायक है, जहाँ डिजिटल शिक्षा के साथ-साथ प्रकृति-आधारित गतिविधियाँ, आउटडोर खेल और सहयोगात्मक शिक्षण को समान प्राथमिकता दी जाती है। भारत में ‘फिट इंडिया मूवमेंट’ और ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020’ जैसे प्रयास इस दिशा में आशाजनक शुरुआत हैं, लेकिन इनका प्रभाव तभी होगा जब इन्हें विद्यालयों, समुदायों और परिवारों तक ठोस रूप में पहुँचाया जाए।
विद्यालयों में पारंपरिक खेलों को पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग बनाना, खेल मैदानों का पुनरुद्धार, और अभिभावकों द्वारा अपने बच्चों के स्क्रीन समय का विवेकपूर्ण नियंत्रण — ये कुछ ऐसे ठोस कदम हैं जो बच्चों को दोबारा संतुलित और सक्रिय बचपन की ओर ले जा सकते हैं। साथ ही, शिक्षा में भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सामाजिक संवाद कौशल को स्थान देना भी समय की आवश्यकता बन चुका है।
बचपन की असली सुंदरता सिर्फ खेलों, या मस्ती के पलों में नहीं है, बल्कि उन क्षणों में है जब बच्चे अपने जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सीखते हैं। वे खेल, मित्रता, प्रतिस्पर्धा और सामूहिकता के माध्यम से अपना व्यक्तित्व गढ़ते हैं, और यही उन्हें जीवन के संघर्षों से निपटने के लिए तैयार करता है। आज, जब तकनीकी दुनिया बच्चों को एकाकी बनाने की चुनौती सामने रख रही है, जब तमाम बच्चे इस आभासी दुनिया में खोये लगते हैं, तो सवाल वाजिब हैं कि क्या हम उस पुरानी खुशबू, उस मिट्टी की महक, उस गिल्ली-डंडे और कंचे के खेल को फिर से लौटा सकते हैं? क्या हम उस गली-मोहल्ले को फिर से जीवित कर सकते हैं, जहाँ बच्चों की हंसी और दौड़-भाग से सजीव था हर एक कोना?
एक देश का भविष्य उसके बच्चों में छुपा होता है। और जब वे अपनी मिट्टी से जुड़कर खेलते हैं, जब वे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, तो न केवल उनका, बल्कि पूरे समाज का भविष्य उज्जवल होता है। यही वह आधार है, जिस पर भारत का समृद्ध और समावेशी समाज खड़ा होगा। यह सामूहिक और साझा ज़िम्मेदारी है — सरकार, समाज और परिवार की — कि बच्चों को एक ऐसा संतुलित और समृद्ध बचपन दें, जहाँ वे तकनीक के साथ-साथ जीवन के वास्तविक पाठ भी सीखें। यदि हम इस संतुलन को साध पाए, तो हम न केवल एक स्वस्थ और सशक्त पीढ़ी तैयार करेंगे, बल्कि हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे, जो अपने मूल्यों, अपनी पहचान और अपनी शक्ति को समझने वाला हो।
संबंधित खबरें
Hindi News / Opinion / डिजिटल दुनिया में सिमटता जा रहा बचपन
यह खबरें भी पढ़ें
लेटेस्ट ओपिनियन न्यूज़
Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.