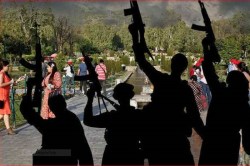Monday, April 28, 2025
इंडियन स्टैडडर्स हैं तो यूरोपियन की बाध्यता क्यों?
—विजय गर्ग
(आर्थिक विशेषज्ञ और भारतीय एवं विदेशी कर प्रणाली के जानकार)
जयपुर•Apr 28, 2025 / 01:51 pm•
विकास माथुर
‘जो पश्चिम का है, वो बेहतर है’ की मानसिकता से आज भी भारत पूरी तरह बाहर निकल नहीं पाया है। इसका एक उदाहरण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में यूरोपियन स्टैंडड्र्स की बढ़ती अनिवार्यता है। इंडियन स्टैंडड्र्स मौजूद होने के बावजूद पिछले तीन दशक से देश में अधिकांश इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में यूरोपियन स्टैंडड्र्स को बाध्य किया जा रहा है, जिससे न केवल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की लागत बढ़ती है, बल्कि टैक्सपेयर्स के पैसों का दुरुपयोग भी हो रहा है। प्राचीन काल से तकनीक के मामले में भारत कहीं से भी पीछे नहीं रहा है। जब दुनिया को इंजीनियरिंग और डिजाइन्स का पूर्ण ज्ञान तक नहीं था, तब से हमारे यहां बांध और इमारतें बनती आ रही हैं।
संबंधित खबरें
यह समय की मांग है कि हम अपने इंडियन स्टैंडड्र्स पर भरोसा जताएं एवं राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर के मानकों के अनुसार, सुरक्षा एवं गुणवत्ता से समझौता न करते हुए समय-समय पर परिवर्तन कर इंडियन स्टैंडड्र्स को अपडेट करें एवं और यूरोपियन स्टैंडड्र्स को नकारें। यह सच है कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी राष्ट्र की आर्थिक तरक्की की रीढ़ होता है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में पिछले दो-ढाई दशक में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में जबर्दस्त तेजी आई है। इस प्रगति के साथ एक नया ट्रेंड भी उभरा है, वो है यूरोपियन स्टैंडड्र्स का बढ़ता उपयोग। हालांकि, यूरोपियन स्टैंडर्ड तकनीकी दृष्टि से उन्नत माने जाते हैं, लेकिन भारत में इनका अंधानुकरण कई स्तरों पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। दरअसल, यूरोपियन स्टैंडड्र्स का विकास यूरोप की जलवायु, भौगोलिक परिस्थितियों और सामाजिक संरचना को ध्यान में रखकर किया गया है, जबकि भारत में जलवायु, मिट्टी की प्रकृति, मानसून की तीव्रता और जनसंख्या घनत्व जैसी स्थितियां बिल्कुल अलग हैं।
ऐसे में यूरोप के ‘वन साइज फिट्स ऑल’ स्टैंडड्र्स को भारत में ज्यों का त्यों लागू करना स्थानीय जरूरतों की उपेक्षा ही तो है। उदाहरण के तौर पर यूरोपियन स्टैंडड्र्स के यूरोकोड के अनुसार डिजाइन किया गया एक फुटब्रिज, जिसका जीवनकाल 100 साल माना जाता है, वो भारत में 20 साल में ही क्षतिग्रस्त हो सकता है, यदि मानसून की तीव्रता, जलभराव और भार क्षमता की गणना स्थानीय रूप से न की जाए। दूसरा, यूरोपियन स्टैंडड्र्स से इंफ्रा प्रोजेक्ट की लागत लगभग दो से तीन गुना तक बढ़ जाती है, जबकि अधिकांश इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सीमित बजट में चलते हैं। ऐसे में यह ओवरडिजाइन और ओवरस्पेंडिंग का केस बन जाता है। विशेषकर सड़क निर्माण और रोपवे प्रोजेक्ट्स में यूरोपियन स्टैंडड्र्स की अनिवार्यता अधिक है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत को अब भी यूरोपियन स्टैंडड्र्स की जरूरत है, जो विकसित देशों की जेब के हिसाब से बने हैं? एक और बात, यूरोपियन स्टैंडड्र्स में कई बार ऐसी तकनीकी शर्तें लगी होती हैं, जो केवल यूरोपियन सप्लायर्स ही पूरा कर सकते हैं। इससे इंडियन इंजीनियरिंग कंपनियों और लघु एवं मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को ठेका मिलना मुश्किल हो जाता है। यह एक तरह का ‘टेक्निकल कॉलोनियलिज्म’ है, जिसमें स्टैंडड्र्स के जरिए बाजार कब्जाया जाता है। फिर यूरोपियन स्टैंडड्र्स के लिए ज्वाइंट वेंचर (जेवी) अनिवार्य हो जाता है एवं इस ज्वाइंट वेंचर के चलते हुए एक मोटी फीस विदेशी कंपनियां ले जाती हैं, जो भी लागत को बढ़ाता है एवं बाद में यह बढ़ी हुई लागत देश की आम जनता से टोल टैक्स या फीस की राशि को बढ़ाकर वसूल की जाती है और देश की आम जनता पर इन यूरोपियन स्टैंडर्ड के कारण सीधा प्रभाव पड़ता है। यूरोपियन स्टैंडड्र्स का असली लाभ तब है, जब प्रोडक्ट्स को यूरोप या इंटरनेशनल मार्केट में बेचना हो, लेकिन अगर प्रोजेक्ट पूरी तरह भारत के उपयोग के लिए है तो क्या यूरोपियन स्टैंडड्र्स का उपयोग उचित है? यूरोपियन स्टैंडड्र्स का चयन ज्ञान से होना चाहिए, न कि दिखावे या विदेशी दबाव से।
भारत की विविध भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थितियों को देखते हुए देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरतें यूरोप या अमरीका से बिल्कुल भिन्न हैं। हमारे देश की जलवायु, भूमि की प्रकृति, जनसंख्या घनत्व, ट्रैफिक पैटर्न और संसाधनों की उपलब्धता विशेष प्रकार की इंजीनियरिंग और डिजाइन दृष्टिकोण की मांग करती है। भारत द्वारा विकसित इंडियन स्टैंडड्र्स (आईएस), इंडियन रोड कांग्रेस (आईआरसी) और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की गाइडलाइन्स एक ऐसी संरचना प्रदान करते हैं, जो स्थानीय जरूरतों, अनुभवों और बजट के अनुसार तैयार की गई है। ये न केवल व्यावहारिक हैं, बल्कि आत्मनिर्भरता और सतत विकास की दिशा में एक मजबूत कदम भी हैं। यूरोपियन स्टैंडड्र्स को सुरक्षा और गुणवत्ता के लिए उच्च माना जाता है, लेकिन इंडियन स्टैंडड्र्स भी देश की भूगोल, मौसम और भूकंपीय क्षेत्रों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। आईएस 456 (कंक्रीट कोड) में भारत की मिट्टी और जलवायु के अनुरूप कंक्रीट डिजाइन के निर्देश हैं। आईआरसी 6 और आईआरसी 112 भारतीय सड़कों, ट्रैफिक और लोडिंग कंडीशन्स के लिए उपयुक्त हैं।
आईएस और आईआरसी कोड्स का निर्माण देश के अनुभवी इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और रिसर्च संस्थानों के सहयोग से हुआ है। इन कोड्स में दशकों के इंडियन प्रोजेक्ट्स का फील्ड अनुभव शामिल है, जो किसी भी विदेशी स्टैंडर्ड में नहीं हो सकता। हालांकि, पहले आईएस कोड्स को अपडेट करने में समय लगता था, लेकिन अब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडड्र्स (बीआईएस) और आईआरसी नियमित रूप से अपने स्टैंडड्र्स को टेक्नोलॉजी और रिसर्च के अनुसार अपडेट कर रहे हैं। इंडियन स्टैंडड्र्स न केवल तकनीकी दृष्टि से मजबूत हैं, बल्कि वे भारत के लिए उपयुक्त, व्यावहारिक और आत्मनिर्भर बनाने वाले हैं।
विडंबना यह है कि ‘आत्मनिर्भर भारत’ की बात करने वाला देश अगर हर बड़े प्रोजेक्ट में यूरोपियन स्टैंडड्र्स, कंसल्टेंट्स और मशीनरी पर निर्भर हो जाए तो यह विरोधाभास नहीं तो और क्या है? सरकार को चाहिए कि वो इंडियन स्टैंडड्र्स की क्षमता को अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी साबित करे। सरकार इंडियन स्टैंडड्र्स को और अधिक वैज्ञानिक, आधुनिक और वैश्विक बनाए, लेकिन अपनी पहचान और जरूरत को खोए बिना, ताकि वो भी यूरोपियन स्टैंडड्र्स से कहीं कमतर नहीं रहें।
Hindi News / Opinion / इंडियन स्टैडडर्स हैं तो यूरोपियन की बाध्यता क्यों?
यह खबरें भी पढ़ें
लेटेस्ट ओपिनियन न्यूज़
Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.