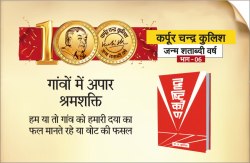Friday, May 2, 2025
बर्नआउट जैसी समस्या से जूझ रहे शिक्षक
डॉ. मोनिका राज
जयपुर•May 01, 2025 / 06:08 pm•
Neeru Yadav
शिक्षक समाज की वह नींव हैं, जिन पर आने वाली पीढ़ियों का भविष्य टिका होता है। वे केवल पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाते, बल्कि बच्चों की सोच, व्यवहार और दृष्टिकोण को आकार देते हैं। एक आदर्श शिक्षक अपने ज्ञान, आचरण और प्रेरणादायक व्यक्तित्व से छात्रों को जीवन के हर मोड़ पर सही राह दिखाता है। परंतु आज के तेजी से बदलते सामाजिक, शैक्षणिक और तकनीकी परिवेश में शिक्षक वर्ग अपने अस्तित्व और मनोबल को लेकर गंभीर संकट से गुजर रहा है। यह संकट केवल संसाधनों या नीतियों का नहीं है, बल्कि एक गंभीर मानसिक और भावनात्मक थकान का है, जिसे हम ‘शिक्षक तनाव’ या ‘बर्नआउट’ के रूप में जानते हैं। यह एक ऐसी परिस्थिति है, जो न केवल शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता, छात्रों के विकास और पूरे समाज की दिशा को भी प्रभावित कर रही है।
शिक्षकों में तनाव और अवसाद का प्रमुख कारण अत्यधिक कार्यभार है। एक शिक्षक की भूमिका अब केवल कक्षा में पढ़ाने तक सीमित नहीं रही है। उन्हें पाठ योजनाएं बनानी होती हैं, मूल्यांकन करना होता है, सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में भाग लेना होता है, तथा प्रशासनिक कार्यों का भी बोझ उठाना पड़ता है। इनमें से अधिकांश कार्य अतिरिक्त समय और मानसिक ऊर्जा की माँग करते हैं। सीमित संसाधनों और समय के भीतर यह सब कुछ करना कई बार असंभव-सा प्रतीत होता है, और यहीं से मानसिक थकान और अवसाद की शुरुआत होती है।
इसके साथ ही एक बड़ी समस्या है- समुचित संसाधनों की कमी। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों या कम वित्तपोषित संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों को पर्याप्त शिक्षण सामग्री, तकनीकी उपकरण या सहायक स्टाफ नहीं मिल पाता। वे चाहकर भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पाते और जब छात्रों की सफलता में बाधा आती है, तो समाज और प्रशासन की अंगुलियां उन्हीं की ओर उठती हैं। कई बार तो उन्हें अपनी जेब से संसाधन जुटाने पड़ते हैं, जिससे न केवल आर्थिक बोझ बढ़ता है बल्कि असंतोष की भावना भी जन्म लेती है।
अवास्तविक अपेक्षाएं भी शिक्षकों को निरंतर मानसिक दबाव में रखती हैं। समाज, अभिभावक और प्रशासक शिक्षकों से यह उम्मीद करते हैं कि वे हर छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकता को समझें, अनुशासन बनाए रखें, परीक्षा परिणाम बेहतर करें और साथ ही विद्यालय की प्रतिष्ठा को भी ऊँचाई तक पहुँचाएँ। परंतु जब उन्हें न तो पर्याप्त समय, संसाधन और सहयोग मिलता है और न ही उचित प्रोत्साहन, तो यह अपेक्षाएँ बोझ का रूप ले लेती हैं। लगातार आलोचना और अपेक्षा का यह दुष्चक्र उन्हें भीतर से तोड़ने लगता है।
कम वेतन और वित्तीय असुरक्षा इस समस्या को और अधिक जटिल बना देती है। अधिकांश देशों, विशेषतः भारत में, शिक्षकों का वेतन अन्य पेशेवरों की तुलना में कम होता है, जबकि उनकी भूमिका कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण होती है। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है, बल्कि आत्म-सम्मान और सामाजिक स्थिति पर भी असर पड़ता है। कई शिक्षक अपनी आजीविका चलाने के लिए अतिरिक्त कार्य करते हैं, जैसे ट्यूशन या पार्ट-टाइम नौकरियां, जिससे उनकी मानसिक और शारीरिक थकावट और बढ़ जाती है।
शिक्षा प्रणाली में बार-बार होने वाले बदलाव भी शिक्षकों की चिंता को बढ़ाते हैं। नई-नई नीतियां, तकनीकी परिवर्तन, पाठ्यक्रमों का पुनर्निर्धारण और मूल्यांकन की विधियां बार-बार बदलती रहती हैं। इससे शिक्षकों को स्वयं को बार-बार ढालना पड़ता है। न केवल उन्हें नए सॉफ्टवेयर और तकनीकी उपकरणों का प्रयोग सीखना पड़ता है, बल्कि उन्हें अपनी शिक्षण शैली भी बार-बार परिवर्तित करनी पड़ती है, जिससे उनका आत्मविश्वास और स्थायित्व प्रभावित होता है।
एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है-कार्य और जीवन में संतुलन की कमी। शिक्षकों की ज़िंदगी में ‘वर्क-लाइफ बैलेंस’ एक सपना बनकर रह गया है। वे विद्यालय से बाहर भी कापियाँ जाँचने, योजनाएँ बनाने और रिपोर्ट तैयार करने में लगे रहते हैं। इस कारण वे अपने परिवार और स्वयं के लिए समय नहीं निकाल पाते, जिससे मानसिक थकान, अकेलापन और असंतोष की भावना गहराती जाती है। यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो डिप्रेशन और बर्नआउट जैसी गंभीर समस्याएँ जन्म लेती हैं।
यह मानसिक और शारीरिक तनाव शिक्षकों के स्वास्थ्य पर गहरा असर डालता है। वे उच्च रक्तचाप, अनिद्रा, थकान, बेचैनी और अन्य शारीरिक बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। मानसिक रूप से वे अवसाद, चिड़चिड़ेपन, हताशा और आत्मग्लानि का अनुभव करते हैं। कई मामलों में यह स्थिति आत्महत्या जैसे खतरनाक कदमों की ओर भी ले जाती है, जो पूरे समाज के लिए चिंताजनक है।
शिक्षकों का यह मानसिक अवसाद उनकी कार्यक्षमता को भी प्रभावित करता है। जब कोई शिक्षक मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है, तो उसमें धैर्य, उत्साह और नवाचार की कमी आ जाती है। वह केवल औपचारिकता निभाने के लिए कक्षा में आता है, जिससे शिक्षण की गुणवत्ता प्रभावित होती है। परिणामस्वरूप छात्र उचित मार्गदर्शन और प्रेरणा से वंचित रह जाते हैं, और शिक्षा की मूल आत्मा खोने लगती है।
इसका सीधा असर छात्रों पर भी पड़ता है। शिक्षक की उदासीनता या तनावपूर्ण व्यवहार से छात्र डरे-सहमे रहते हैं। उनकी सीखने की क्षमता, आत्मविश्वास और विद्यालय के प्रति रुचि प्रभावित होती है। एक तनावग्रस्त शिक्षक कभी भी एक प्रेरक वातावरण नहीं बना सकता, जो कि शिक्षा के लिए अनिवार्य होता है। यह स्थिति तब और भयावह हो जाती है जब शिक्षक इस पेशे को छोड़ने का निर्णय लेने लगते हैं। कई योग्य और अनुभवी शिक्षक या तो समय से पहले सेवानिवृत्ति ले लेते हैं या फिर किसी अन्य पेशे में चले जाते हैं, जिससे शिक्षा व्यवस्था को भारी नुकसान होता है। यह न केवल ज्ञान की हानि है, बल्कि अनुभव, मार्गदर्शन और अनुशासन की भी क्षति है, जिसका प्रभाव दीर्घकालिक होता है।
इस स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक है कि हम शिक्षकों के कार्यभार को व्यवस्थित करें। विद्यालय प्रशासन को चाहिए कि अनावश्यक प्रशासनिक कार्यों को कम किया जाए और शिक्षकों को उनकी मुख्य भूमिका शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर दिया जाए। साथ ही उन्हें पर्याप्त सहायक स्टाफ और तकनीकी संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएँ, जिससे उनका काम सरल और प्रभावी बन सके।
सरकार को शिक्षकों के वेतन और भत्तों में सुधार करना चाहिए। आर्थिक सुरक्षा मिलने से न केवल उनका आत्मसम्मान बढ़ेगा, बल्कि वे पूरी निष्ठा और ऊर्जा के साथ अपने कार्य में लगे रहेंगे। इसके अलावा, मानसिक स्वास्थ्य के लिए परामर्श सेवाएँ, योग, ध्यान और तनाव प्रबंधन कार्यशालाएँ नियमित रूप से आयोजित की जानी चाहिएं, ताकि वे अपने मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल कर सकें।
विद्यालयों को एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सहयोग, संवाद और सहानुभूति हो। शिक्षकों को यह महसूस होना चाहिए कि वे अकेले नहीं हैं और उनके सहकर्मी तथा प्रशासन उनके साथ हैं। इससे उनके आत्मबल और मनोबल में वृद्धि होगी। साथ ही प्रशिक्षण और कार्यशालाओं के माध्यम से उन्हें नवीनतम तकनीकों और विधियों से अवगत कराया जाए, जिससे उनकी शिक्षा में रुचि और नवाचार की भावना बनी रहे।
शिक्षकों को भी अपने जीवन में संतुलन बनाने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें अपने लिए समय निकालना चाहिए, परिवार और मित्रों के साथ समय बिताना चाहिए और अपने शौक या रुचियों को विकसित करना चाहिए। यह मानसिक सुकून और संतुलन की दृष्टि से आवश्यक है।
हमें यह समझना होगा कि शिक्षक केवल ज्ञान का स्रोत नहीं हैं, वे समाज की आत्मा हैं। यदि उनका मनोबल, मानसिक स्वास्थ्य और संतुलन ठीक नहीं रहेगा, तो हम एक स्वस्थ, शिक्षित और प्रगतिशील समाज की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए यह समय की माँग है कि हम शिक्षकों को वह सम्मान, सहयोग और संसाधन प्रदान करें जिसके वे वास्तविक अधिकारी हैं। केवल एक स्वस्थ, प्रेरित और संतुष्ट शिक्षक ही राष्ट्र की भावी पीढ़ी को श्रेष्ठ मार्ग दिखा सकता है। अतः शिक्षक तनाव और अवसाद की समस्या को हमें एक सामाजिक उत्तरदायित्व की तरह गंभीरता से लेना होगा। यही समाज के भविष्य की सच्ची रक्षा होगी।
शिक्षकों में तनाव और अवसाद का प्रमुख कारण अत्यधिक कार्यभार है। एक शिक्षक की भूमिका अब केवल कक्षा में पढ़ाने तक सीमित नहीं रही है। उन्हें पाठ योजनाएं बनानी होती हैं, मूल्यांकन करना होता है, सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में भाग लेना होता है, तथा प्रशासनिक कार्यों का भी बोझ उठाना पड़ता है। इनमें से अधिकांश कार्य अतिरिक्त समय और मानसिक ऊर्जा की माँग करते हैं। सीमित संसाधनों और समय के भीतर यह सब कुछ करना कई बार असंभव-सा प्रतीत होता है, और यहीं से मानसिक थकान और अवसाद की शुरुआत होती है।
इसके साथ ही एक बड़ी समस्या है- समुचित संसाधनों की कमी। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों या कम वित्तपोषित संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों को पर्याप्त शिक्षण सामग्री, तकनीकी उपकरण या सहायक स्टाफ नहीं मिल पाता। वे चाहकर भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पाते और जब छात्रों की सफलता में बाधा आती है, तो समाज और प्रशासन की अंगुलियां उन्हीं की ओर उठती हैं। कई बार तो उन्हें अपनी जेब से संसाधन जुटाने पड़ते हैं, जिससे न केवल आर्थिक बोझ बढ़ता है बल्कि असंतोष की भावना भी जन्म लेती है।
अवास्तविक अपेक्षाएं भी शिक्षकों को निरंतर मानसिक दबाव में रखती हैं। समाज, अभिभावक और प्रशासक शिक्षकों से यह उम्मीद करते हैं कि वे हर छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकता को समझें, अनुशासन बनाए रखें, परीक्षा परिणाम बेहतर करें और साथ ही विद्यालय की प्रतिष्ठा को भी ऊँचाई तक पहुँचाएँ। परंतु जब उन्हें न तो पर्याप्त समय, संसाधन और सहयोग मिलता है और न ही उचित प्रोत्साहन, तो यह अपेक्षाएँ बोझ का रूप ले लेती हैं। लगातार आलोचना और अपेक्षा का यह दुष्चक्र उन्हें भीतर से तोड़ने लगता है।
कम वेतन और वित्तीय असुरक्षा इस समस्या को और अधिक जटिल बना देती है। अधिकांश देशों, विशेषतः भारत में, शिक्षकों का वेतन अन्य पेशेवरों की तुलना में कम होता है, जबकि उनकी भूमिका कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण होती है। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है, बल्कि आत्म-सम्मान और सामाजिक स्थिति पर भी असर पड़ता है। कई शिक्षक अपनी आजीविका चलाने के लिए अतिरिक्त कार्य करते हैं, जैसे ट्यूशन या पार्ट-टाइम नौकरियां, जिससे उनकी मानसिक और शारीरिक थकावट और बढ़ जाती है।
शिक्षा प्रणाली में बार-बार होने वाले बदलाव भी शिक्षकों की चिंता को बढ़ाते हैं। नई-नई नीतियां, तकनीकी परिवर्तन, पाठ्यक्रमों का पुनर्निर्धारण और मूल्यांकन की विधियां बार-बार बदलती रहती हैं। इससे शिक्षकों को स्वयं को बार-बार ढालना पड़ता है। न केवल उन्हें नए सॉफ्टवेयर और तकनीकी उपकरणों का प्रयोग सीखना पड़ता है, बल्कि उन्हें अपनी शिक्षण शैली भी बार-बार परिवर्तित करनी पड़ती है, जिससे उनका आत्मविश्वास और स्थायित्व प्रभावित होता है।
एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है-कार्य और जीवन में संतुलन की कमी। शिक्षकों की ज़िंदगी में ‘वर्क-लाइफ बैलेंस’ एक सपना बनकर रह गया है। वे विद्यालय से बाहर भी कापियाँ जाँचने, योजनाएँ बनाने और रिपोर्ट तैयार करने में लगे रहते हैं। इस कारण वे अपने परिवार और स्वयं के लिए समय नहीं निकाल पाते, जिससे मानसिक थकान, अकेलापन और असंतोष की भावना गहराती जाती है। यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो डिप्रेशन और बर्नआउट जैसी गंभीर समस्याएँ जन्म लेती हैं।
यह मानसिक और शारीरिक तनाव शिक्षकों के स्वास्थ्य पर गहरा असर डालता है। वे उच्च रक्तचाप, अनिद्रा, थकान, बेचैनी और अन्य शारीरिक बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। मानसिक रूप से वे अवसाद, चिड़चिड़ेपन, हताशा और आत्मग्लानि का अनुभव करते हैं। कई मामलों में यह स्थिति आत्महत्या जैसे खतरनाक कदमों की ओर भी ले जाती है, जो पूरे समाज के लिए चिंताजनक है।
शिक्षकों का यह मानसिक अवसाद उनकी कार्यक्षमता को भी प्रभावित करता है। जब कोई शिक्षक मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है, तो उसमें धैर्य, उत्साह और नवाचार की कमी आ जाती है। वह केवल औपचारिकता निभाने के लिए कक्षा में आता है, जिससे शिक्षण की गुणवत्ता प्रभावित होती है। परिणामस्वरूप छात्र उचित मार्गदर्शन और प्रेरणा से वंचित रह जाते हैं, और शिक्षा की मूल आत्मा खोने लगती है।
इसका सीधा असर छात्रों पर भी पड़ता है। शिक्षक की उदासीनता या तनावपूर्ण व्यवहार से छात्र डरे-सहमे रहते हैं। उनकी सीखने की क्षमता, आत्मविश्वास और विद्यालय के प्रति रुचि प्रभावित होती है। एक तनावग्रस्त शिक्षक कभी भी एक प्रेरक वातावरण नहीं बना सकता, जो कि शिक्षा के लिए अनिवार्य होता है। यह स्थिति तब और भयावह हो जाती है जब शिक्षक इस पेशे को छोड़ने का निर्णय लेने लगते हैं। कई योग्य और अनुभवी शिक्षक या तो समय से पहले सेवानिवृत्ति ले लेते हैं या फिर किसी अन्य पेशे में चले जाते हैं, जिससे शिक्षा व्यवस्था को भारी नुकसान होता है। यह न केवल ज्ञान की हानि है, बल्कि अनुभव, मार्गदर्शन और अनुशासन की भी क्षति है, जिसका प्रभाव दीर्घकालिक होता है।
इस स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक है कि हम शिक्षकों के कार्यभार को व्यवस्थित करें। विद्यालय प्रशासन को चाहिए कि अनावश्यक प्रशासनिक कार्यों को कम किया जाए और शिक्षकों को उनकी मुख्य भूमिका शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर दिया जाए। साथ ही उन्हें पर्याप्त सहायक स्टाफ और तकनीकी संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएँ, जिससे उनका काम सरल और प्रभावी बन सके।
सरकार को शिक्षकों के वेतन और भत्तों में सुधार करना चाहिए। आर्थिक सुरक्षा मिलने से न केवल उनका आत्मसम्मान बढ़ेगा, बल्कि वे पूरी निष्ठा और ऊर्जा के साथ अपने कार्य में लगे रहेंगे। इसके अलावा, मानसिक स्वास्थ्य के लिए परामर्श सेवाएँ, योग, ध्यान और तनाव प्रबंधन कार्यशालाएँ नियमित रूप से आयोजित की जानी चाहिएं, ताकि वे अपने मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल कर सकें।
विद्यालयों को एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सहयोग, संवाद और सहानुभूति हो। शिक्षकों को यह महसूस होना चाहिए कि वे अकेले नहीं हैं और उनके सहकर्मी तथा प्रशासन उनके साथ हैं। इससे उनके आत्मबल और मनोबल में वृद्धि होगी। साथ ही प्रशिक्षण और कार्यशालाओं के माध्यम से उन्हें नवीनतम तकनीकों और विधियों से अवगत कराया जाए, जिससे उनकी शिक्षा में रुचि और नवाचार की भावना बनी रहे।
शिक्षकों को भी अपने जीवन में संतुलन बनाने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें अपने लिए समय निकालना चाहिए, परिवार और मित्रों के साथ समय बिताना चाहिए और अपने शौक या रुचियों को विकसित करना चाहिए। यह मानसिक सुकून और संतुलन की दृष्टि से आवश्यक है।
हमें यह समझना होगा कि शिक्षक केवल ज्ञान का स्रोत नहीं हैं, वे समाज की आत्मा हैं। यदि उनका मनोबल, मानसिक स्वास्थ्य और संतुलन ठीक नहीं रहेगा, तो हम एक स्वस्थ, शिक्षित और प्रगतिशील समाज की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए यह समय की माँग है कि हम शिक्षकों को वह सम्मान, सहयोग और संसाधन प्रदान करें जिसके वे वास्तविक अधिकारी हैं। केवल एक स्वस्थ, प्रेरित और संतुष्ट शिक्षक ही राष्ट्र की भावी पीढ़ी को श्रेष्ठ मार्ग दिखा सकता है। अतः शिक्षक तनाव और अवसाद की समस्या को हमें एक सामाजिक उत्तरदायित्व की तरह गंभीरता से लेना होगा। यही समाज के भविष्य की सच्ची रक्षा होगी।
संबंधित खबरें
Hindi News / Opinion / बर्नआउट जैसी समस्या से जूझ रहे शिक्षक
यह खबरें भी पढ़ें
लेटेस्ट ओपिनियन न्यूज़
Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.