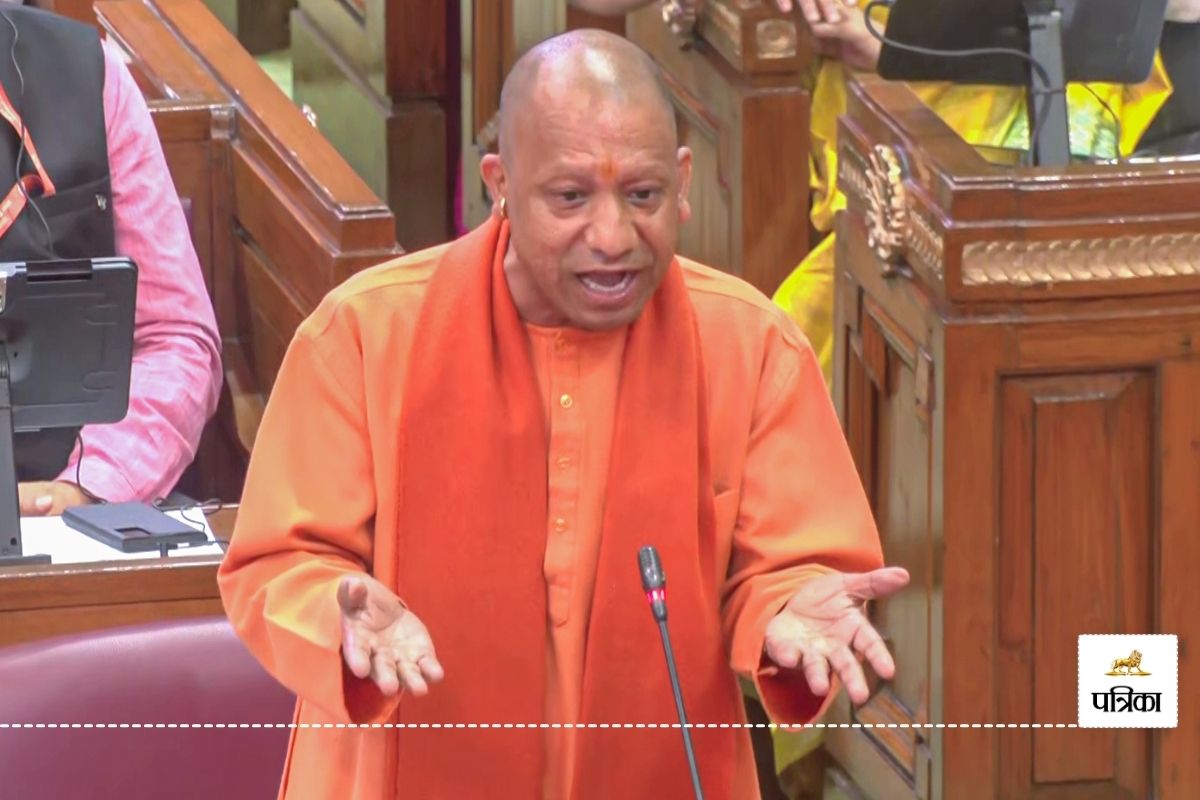वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में निपट आय (disposable income) और वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख कर रियायतें पेश की गईं। आयकर छूट की सीमा ₹7 लाख से बढ़कर ₹12 लाख हो गई है, जिसमें वेतनभोगी करदाताओं को ₹75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा। 30% कर दर अब 24 लाख रुपए से अधिक की आय पर लागू होती है, जो मध्यम और उच्च आय वालों के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करेगा। वरिष्ठ नागरिकों की ब्याज आय छूट दोगुनी होकर ₹1 लाख की गई। कर अनुपालन को अधिक सरल करने से, कर दाखिल करने की प्रक्रिया आसान और प्रभावी होने की संभावना बनती है। ये उपाय उपभोग, बचत और निवेश को बढ़ावा देते हैं, जो आर्थिक वृद्धि बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
बिना जोखिम के राहत: कर कटौती और वित्तीय स्थिरता का संतुलन प्रत्यक्ष कर (डायरेक्ट टैक्स) में ₹1 लाख करोड़ और अप्रत्यक्ष कर (इन्डायरेक्ट टैक्स) में 2,600 करोड़ रुपए के वार्षिक राजस्व नुकसान के बावजूद, वित्तीय घाटा घटाकर 4.4% (FY26) किया गया है, जबकि अभी यह 4.8% है। यह घाटा अधिक ऋण लेने के परिणामस्वरूप नहीं, बल्कि कुशल व्यय कटौती और निजी क्षेत्र की भागीदारी के कारण नियंत्रित किया गया है।
सरकार का ध्यान अवसंरचना, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के लक्षित निवेश पर केंद्रित है। 10.8 लाख करोड़ रुपए की राशि सड़क, रेलवे और बंदरगाहों के लिए आवंटित की गई है, जबकि 10,000 करोड़ रुपए स्टार्टअप के लिए निर्धारित किए गए हैं – इससे यह स्पष्ट होता है कि बजट दीर्घकालिक विकास-उन्मुख रणनीति पर केंद्रित है, न कि अल्पकालिक राजस्व संग्रह पर।
हालांकि, अवसंरचना क्षेत्र का कुल आवंटन 11.21 लाख करोड़ रुपए है, जो पिछले वर्ष के 11.11 लाख करोड़ रुपए की तुलना में केवल 0.9% अधिक है। इसके बावजूद, सरकार ने केंद्रीय निवेश के बजाय राज्य-नेतृत्व वाली पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) नीति अपनाई है। 1.5 लाख करोड़ रुपए की 50 वर्षीय ब्याज-मुक्त ऋण योजना राज्यों को पूंजीगत परियोजनाओं और आवश्यक सुधारों के लिए दी गई है, जिससे उनके राजकोषीय घाटे-जीएसडीपी (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) अनुपात में कमी आने, तथा आर्थिक विकास में आगे निवेश को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।
वित्त वर्ष 2025 के बजट अनुमान के अनुसार, 9.2 लाख करोड़ रुपए की राज्य पूंजीगत व्यय के परिणामस्वरूप ₹10 लाख करोड़ का बजट घाटा हुआ (चित्र 1), जो राज्य के जीडीपी का 3.2% है (NSE, 2024)। केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए अतिरिक्त राज्य व्यय से कुल पूंजीगत व्यय में सुधार होने की संभावना है, वो भी बिना वित्तीय घाटे के, क्योंकि यह ऋण ब्याज मुक्त है। इसके अतिरिक्त, यह वित्त पोषण बहुगुणक प्रभाव (मल्टीप्लायर इफेक्ट) उत्पन्न कर सकता है, जो आमतौर पर भारत में 2.5-3 गुना जीडीपी विस्तार करता है, जिससे उच्च आर्थिक उत्पादन और दीर्घकालिक राजस्व सृजन को बढ़ावा मिलेगा। अन्य विकल्पों से उधारी पर निर्भरता घटने से राज्यों के वित्तीय घाटे-से-जीडीपी अनुपात में सुधार होने की संभावना है।
राजकोषीय घाटे में सुधार के अलावा, यह आवंटन क्षेत्रीय सरकारों को केंद्र द्वारा निर्धारित विकास मार्ग के बजाय, उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने वाली परियोजनाओं को विकसित करने में अतिरिक्त स्वतंत्रता प्रदान करती है। इससे क्षेत्रीय आर्थिक दक्षता बढ़ती है और आर्थिक लाभ के लिए संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है।
सरकार ने व्यापक सब्सिडी से होने वाली अक्षमताओं को रोकते हुए खाद्य और उर्वरक सब्सिडी को पुनर्गठित किया है ताकि वे जरूरतमंदों तक ही सीमित रहें। सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल को बढ़ावा देने से सरकार का वित्तीय बोझ कम होने की आशंका है, क्योंकि निजी निवेशक अब बड़ी परियोजनाओं के वित्तपोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रशासनिक लागत युक्तिकरण, सुव्यवस्थित सब्सिडी और निजी भागीदारी से राजकोषीय अनुशासन और आर्थिक विस्तार में संतुलन बना रहेगा। जैसे-जैसे निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ेगी, सरकारी संसाधन अधिक प्रभावी ढंग से उच्च-मूल्य क्षेत्रों में निवेश किए जा सकेंगे, जिससे कर बोझ कम रहते हुए दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित होगी।
क्या कर राहत निवेश और औद्योगिक विस्तार को गति दे सकती है? भारत ने हाल ही में एक कठिन तिमाही का सामना किया, जब जुलाई-सितंबर FY25 में जीडीपी वृद्धि घटकर 5.4% रह गई, जो पिछले सात तिमाहियों का सबसे निचला स्तर है। 2030 तक अपने मौजूदा आर्थिक आकार से दोगुनी वृद्धि के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की महत्वाकांक्षा केवल 11% की दोहरे अंकों वाली वार्षिक नाममात्र जीडीपी वृद्धि दर के साथ ही प्राप्त की जा सकती है, बशर्ते कि मुद्रास्फीति 3-4% की सीमा में बनी रहे।
बजट में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम और स्टार्टअप को प्राथमिकता दी गई है, लेकिन गैर- MSME क्षेत्र के लिए बहुत कम प्रावधान किए गए हैं, जो भारत के सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) में 70% का योगदान देता है। इसकी वृद्धि उपभोक्ता वस्तुओं की मांग पर निर्भर करती है, लेकिन यह पक्ष भी अकेले बड़े पैमाने पर निजी क्षेत्र के निवेश को गति देने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है; यह काफी हद तक मौजूदा व्यावसायिक विश्वास पर निर्भर करता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 की समीक्षा से पता चलता है कि भारत में व्यावसायिक विश्वास मजबूत बना हुआ है, और विकास अपने दशकीय औसत 6-7% के काफी करीब है।
भारत का सेवा क्षेत्र मजबूत बना हुआ है, HSBC इंडिया परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) लगातार 41 महीनों से विस्तार की दिशा में है, जिसका मूल्य FY25 के पहले पाँच महीनों में 60 से ऊपर रहा। यह मज़बूत उपभोक्ता वस्तुओं की मांग की ओर संकेत देता है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के बीच दोहरे अंकों की ऋण वृद्धि मजबूत ऋण प्रवृत्तियों को दर्शाती है, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) निवेशक आधार तीन गुना बढ़कर अगस्त 2024 में 10 करोड़ को पार कर गया। इसके अतिरिक्त, डीमैट खातों में 33% की वार्षिक वृद्धि, 12 साल के निम्नतम 2.6% सकल गैर-निष्पादित आस्तियों (जीएनपीए) अनुपात और 27.1 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार भारत की व्यापक आर्थिक स्थिरता को दर्शाता है।
निष्कर्ष केंद्रीय बजट 2025 कर राहत प्रदान करते हुए वित्तीय स्थिरता बनाए रखता है। हालांकि, विकसित भारत 2047 की ओर बढ़ने के लिए केवल कर रियायतों और अवसंरचना निवेश पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा। इस लक्ष्य की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि निजी क्षेत्र इस अवसर का उपयोग करके रोजगार सृजन, उत्पादकता वृद्धि और विनिर्माण क्षमता का विस्तार कैसे करता है।
उपभोक्ता व्यवहार भी एक महत्वपूर्ण कारक रहेगा। घरेलू आय का उपभोग, बचत और उच्च गुणक क्षेत्रों में निवेश के बीच संतुलन औद्योगिक विस्तार और स्थायी आर्थिक वृद्धि को प्रभावित करेगा। यह सुनिश्चित करना कि बढ़ी हुई निपट आय (disposable income) उत्पादक आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तित हो, भारत के दीर्घकालिक विकास पथ को निर्धारित करेगा।